मित्रों आप सभी लोगों को नमस्कार कबीर के दोहे सम्पूर्ण 54000 शब्दों में Part-1 (kabir ke dohe) इस ब्लॉग पोस्ट पर आपको मिलेगा,ब्लॉग वेबपेज पर स्पीड से दिखे जिससे आप लोगों को सुविधा हो इसलिए इसे 7 पार्ट में बनाया गया है.
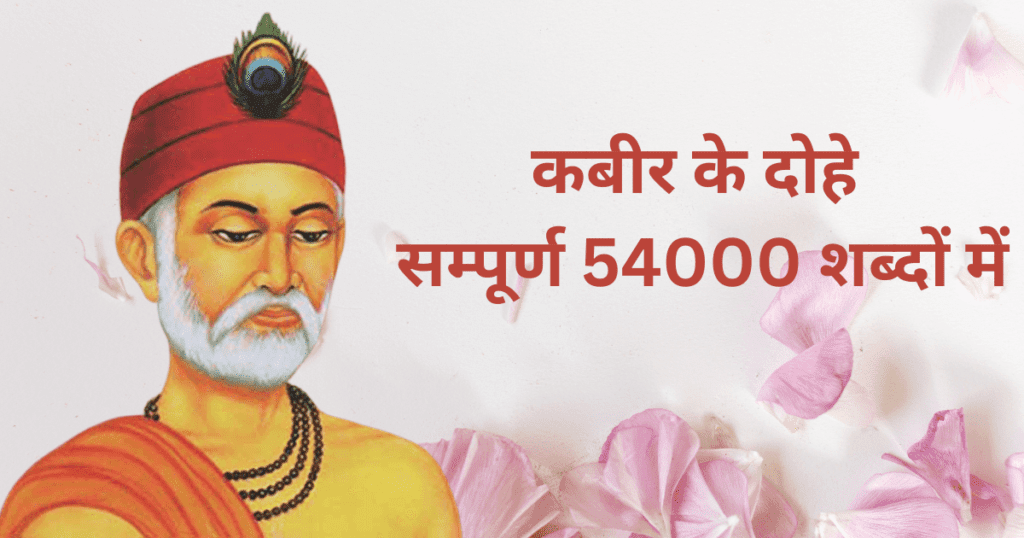
साखी – गुरुदेव को अंग,कबीर के दोहे सम्पूर्ण 54000 शब्दों में
सतगुर सवाँन को सगा, सोधी सईं न दाति।
हरिजी सवाँन को हितू, हरिजन सईं न जाति॥1॥
अर्थ- इस पंक्ति में कहा गया है कि सतगुर (सत्पुरुष या गुरु) सभी को जानता है और उनकी कृपा से ही आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। आत्मा खोजने का मार्ग सतगुर के माध्यम से ही संभव है। सतगुर के माध्यम से हरिजी (भगवान) की सेवा करने का महत्व बताया गया है। यहां यह भी कहा जाता है कि सतगुर के साथ ही सभी लोग समान होते हैं, जन्म-जाति का कोई महत्व नहीं रखता।
बलिहारी गुर आपणैं द्यौं हाड़ी कै बार।
जिनि मानिष तैं देवता, करत न लागी बार॥2॥
अर्थ-श्रद्धाभक्ति और गुरु के प्रति कृतज्ञता का अभिवादन है। “बलिहारी” का अर्थ होता है “बड़ी भाग्यशाली” या “बड़ी कृतज्ञता”। यहां भक्त गुरु की महत्वपूर्णता को मानता है और उनकी सेवा करने में अपनी अद्वितीय भाग्यशालीता को स्वीकार करता है। “आपणैं द्यौं हाड़ी कै बार” का अर्थ है कि गुरु की सेवा करना बड़ी भाग्यशालीता है, जो आत्मा को मुक्ति की दिशा में ले जा सकता है। जो व्यक्ति गुरु की सेवा करता है, वह वास्तव में देवता के समान हो जाता है और उस पर कोई दुर्बलता नहीं होती। “देवता” शब्द यहां दिखावा करता है कि गुरु आत्मा को उच्चतम आदर्शों और दिव्यता की दिशा में प्रेरित करने में मदद करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि गुरु की सेवा में आत्मा को अनंत सत्य का अनुभव होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
सतगुर की महिमा, अनँत, अनँत किया उपगार।
लोचन अनँत उघाड़िया, अनँत दिखावणहार॥3॥
अर्थ- यह एक प्रशंसा (भक्ति) कविता का शुरुआती भाग है, जो एक सतगुरु की महिमा को स्तुति करने के लिए है। इसमें सतगुरु की अद्वितीयता और उसकी अनंत गुणगान किया गया है। इस प्रकार की कविताएँ आमतौर पर भक्ति और आत्मा के साथ दिव्य जीवन की ऊँचाईयों की ओर प्रेरित करने के लिए लिखी जाती हैं।सतगुरु की महिमा” का मतलब है कि सतगुरु की अद्वितीयता और महिमा अनंत (अविच्छिन्न और अनंत) हैं। “लोचन अनँत उघाड़िया” में इसका वर्णन है कि सतगुरु की आंखें अनंत की ओर हैं, और वह अनंत की गहराईयों को देख सकते हैं। “अनँत दिखावणहार” में यह कहा गया है कि सतगुरु वह दिखावणहार हैं जो अनंत को हमें दिखा सकते हैं, अर्थात् वे अनंत ब्रह्म को हमारे सामने प्रकट कर सकते हैं।
राम नाम के पटतरे, देबे कौ कुछ नाहिं।
क्या ले गुर सन्तोषिए, हौंस रही मन माहिं॥4॥
अर्थ-भगवान राम के नाम की रौंगत में कोई भी दुर्बलता या कमी नहीं है, और उनके नाम की महिमा अत्यंत उच्च है। यह कविता बता रही है कि भगवान के नाम में कोई असमर्थता या अभाव नहीं है।गुरु और संतों को क्या मिलता है? और उसका उत्तर है कि वह आत्मसंतोष है, जिससे मन को सुख मिलता है। इसमें यह भी सूचित है कि भक्ति में लगे रहने से मन सुखी रहता है।
सतगुर के सदकै करूँ, दिल अपणी का साछ।
सतगुर हम स्यूँ लड़ि पड़ा महकम मेरा बाछ॥5॥
अर्थ-सतगुरु की सेवा करना और उसके मार्ग पर चलना, दिल की सच्चाई से किया जाए। यानी, यह भक्ति और सेवा दिल से होनी चाहिए।सतगुरु के मार्ग पर चलते हुए, भक्त अपनी आत्मा के महकम (आत्मा के अद्वितीयता का अनुभव) में लड़ाई लड़ रहा है, और इससे उसकी आत्मा का उद्धार हो रहा है। “महकम मेरा बाछ” में “बाछ” का अर्थ होता है सागर या बारिश, जिससे आत्मा को शुद्धि मिलती है।
सतगुर लई कमाँण करि, बाँहण लागा तीर।
एक जु बाह्यां प्रीति सूँ, भीतरि रह्या सरीर॥6॥
अर्थ-इसमें यह कहा जा रहा है कि सतगुरु की सेवा करना, उसके लिए काम करना, व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुँचाने में मदद करता है। “बाँहण लागा तीर” में यह बताया गया है कि यह सतगुरु के मार्ग पर चलने में सहारा प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सजग रहता है।भक्ति में लगे रहने से व्यक्ति बाहरी और भीतरी प्रेम में लगा रहता है। उसका शरीर भी इस प्रेम में समर्पित हो जाता है। इससे यह भी सूचित होता है कि सतगुरु की सेवा और उसके मार्ग पर चलने से भक्ति में आत्मिक समृद्धि होती है।
सतगुर साँवा सूरिवाँ, सबद जू बाह्या एक।
लागत ही में मिलि गया, पढ़ा कलेजै छेक॥7॥
अर्थ- सतगुरु सूर्य की तरह सबको प्रकाशित करने वाले हैं और उनका सबद (उपदेश या बाणी) हमें एकता में मिला देता है।सतगुरु से मिलना और उनके साथ बनी रहना अत्यंत सरल है, जिससे भक्त को आत्मा का अनुभव होता है। “पढ़ा कलेजै छेक” में इसका तात्पर्य है कि सतगुरु की बाणी या उपदेश से आत्मा को शुद्धि मिलती है, जैसे कि शिक्षा कलेज में होती है और वह छेक (साफी) का कार्य करती है।
सतगुर मार्या बाण भरि, धरि करि सूधी मूठि।
अंगि उघाड़ै लागिया, गई दवा सूँ फूंटि॥8॥
अर्थ-सतगुरु ने अपने उपदेशों के बाणों से भरा हुआ है, जिससे भक्त ने अपनी आत्मा को सुधार लिया है। “धरि करि सूधी मूठि” में यह बताया गया है कि भक्त ने उन उपदेशों को अपनी आत्मा में स्थान दिया और उन्हें पूरी तरह से अपनाया हैसतगुरु के उपदेशों का अनुसरण करते हुए, भक्त ने अपने अंगों (शरीर) की उघाड़ाई (शुद्धि की प्रक्रिया) की है और उससे उसका रोग दूर हो गया है। “गई दवा सूँ फूंटि” में इसका अर्थ है कि उसने वह औषधि पूरी तरह से प्राप्त कर ली है और उससे उसकी आत्मा में शुद्धि हो रही है।
हँसै न बोलै उनमनी, चंचल मेल्ह्या मारि।
कहै कबीर भीतरि भिद्या, सतगुर कै हथियार॥9॥
अर्थ-जो व्यक्ति अचेतन है और ज्यों ही उसका मन चंचल होता है, वह बोलना बंद कर देता है और उसका मन मेल्हों (चंचलता) में रहता है।संत कबीर यह कह रहे हैं कि उन्होंने अपने भीतर एक गुप्त रहस्य को खोज लिया है, और इसे खोलने के लिए उनके पास सतगुरु का उपदेश और गुरु की शक्ति है। इससे यह भी सूचित होता है कि सतगुरु का हथियार अत्यंत महत्वपूर्ण है जो व्यक्ति को आत्मा के आद्यात्मिक रहस्यों को समझने में सहारा प्रदान करता है।
गूँगा हूवा बावला, बहरा हुआ कान।
पाऊँ थै पंगुल भया, सतगुर मार्या बाण॥10॥
अर्थ-जो व्यक्ति मूक हो गया है (गूँगा हूवा), और उसके कान बहरे हो गए हैं (बावला)। यह बयान करता है कि ऐसा व्यक्ति आत्मा के आद्यात्मिक ज्ञान से वंचित हो गया है,जब व्यक्ति को अपने पैरों में पंगुल आ गई (पाऊँ थै पंगुल भया), तब सतगुरु ने अपने उपदेश के बाण से उसे मारा (समझाया या शिक्षा दी)। इससे यह बताता है कि सतगुरु के उपदेश से ही व्यक्ति को आत्मा के आद्यात्मिक ज्ञान का अनुभव होता है और उसकी आत्मा को आध्यात्मिक रूप से सुधार होता है।
पीछे लागा जाइ था, लोक वेद के साथि।
आगै थैं सतगुर मिल्या, दीपक दीया हाथि॥11॥
अर्थ-कई लोग पुराने धार्मिक शास्त्रों के साथ चल रहे थे या उनकी अनुयायी थे,आगे जाकर उन्होंने सतगुरु को मिला और उसने उन्हें एक दीपक (प्रकाश) दिया है, जो कि हाथी के समान भारी और महत्वपूर्ण है। यह बयान करता है कि सतगुरु के उपदेश और गुरु की शिक्षा व्यक्ति के जीवन में प्रकाश और मार्गदर्शन का कारण होती है।
दीपक दीया तेल भरि, बाती दई अघट्ट।
पूरा किया बिसाहूणाँ, बहुरि न आँवौं हट्ट॥12॥
अर्थ-जब दीपक में तेल भरा जाता है, तो उसकी बाती (बत्ती) बन जाती है और वह अघट्ट (अटल और अच्छी तरह से जलने वाली) होती है।समस्त को पूरा करने के बाद, दीपक बहुत दिनों तक नहीं बुझता है, यानी कि उसकी आत्मा का प्रकाश बहुत दिनों तक बना रहता है और कभी नहीं हटेगा.
ग्यान प्रकास्या गुर मिल्या, सो जिनि बीसरि जाइ।
जब गोबिंद कृपा करी, तब गुर मिलिया आइ॥13॥
अर्थ- जिनको ज्ञान का प्रकाश मिलता है, वही व्यक्ति समझता है कि सब कुछ उसी में है और उसे गुरु का आवश्यकता नहीं होती।जब गोबिंद (ईश्वर) कृपा करता है, तब ही कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक सार्वभौमिक गुरु से मिलता है और उसे आत्मा का अद्वितीयता का अनुभव होता है।
कबीर गुर गरवा मिल्या, रलि गया आटैं लूँण।
जाति पाँति कुल सब मिटै, नांव धरोगे कौण॥14॥
अर्थ-संत कबीर जी को गुरु की कृपा मिली है, जिससे उनकी आता (गेहूं की बौणी) और लूँण (नमक) मिल गया है, यानी उनका जीवन समृद्धि और पूर्णता से भर गया है,जब गुरु की कृपा मिलती है, तो सभी जातियाँ, पाँतियाँ, और कुल समाप्त हो जाते हैं, और फिर व्यक्ति को अपना नाम कैसे धारण करना चाहिए, यह सवाल उठता है।
जाका गुर भी अंधला, चेला खरा निरंध।
अंधा अंधा ठेलिया, दून्यूँ कूप पड़ंत॥15॥
अर्थ- जिसका गुरु भी अंधा है, और उसका चेला बहुत ईमानदार और निष्कलंक (निरंध) है। यह बताता है कि अगर गुरु भी अंधा है तो भी शिष्य को आत्मा के आद्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति में सफलता मिल सकती है। अंधा व्यक्ति अंधविश्वास में फंसा होता है और वह अपने अज्ञान के कूप में गिर जाता है। इससे यह सिखने को मिलता है कि आत्मा को समझने और आत्मिक सुधार के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, और गुरु की शिक्षा का महत्वपूर्ण होना चाहिए।
नाँ गुर मिल्या न सिष भया, लालच खेल्या डाव।
दुन्यूँ बूड़े धार मैं, चढ़ि पाथर की नाव॥16॥
अर्थ- जिसको गुरु नहीं मिला है और जो सिष्य नहीं बना है, वह लालच में डूबा हुआ है और अविवेक में फंसा हुआ है। यह बताता है कि गुरु की शिक्षा के बिना व्यक्ति आत्मिक सुधार करने में सक्षम नहीं हो सकता है।इस संसार में (दुनिया बूड़े धार में), जो व्यक्ति चढ़ी पथर की नाव पर बैठा है, वह आत्मिक सुधार का मार्ग नहीं चुन पा रहा है, और वह अज्ञान और लालच में डूबा हुआ है।
चौसठ दीवा जोइ करि, चौदह चन्दा माँहि।
तिहिं धरि किसकौ चानिणौं, जिहि घरि गोबिंद नाहिं॥17॥
अर्थ-चौसठ दीपक जलाकर, चौदह चाँदों के महीने में।तीनों धरती किसकी चमक को चाहें, जिस घर में गोविंद नहीं है।
निस अधियारी कारणैं, चौरासी लख चंद।
अति आतुर ऊदै किया, तऊ दिष्टि नहिं मंद॥18॥
अर्थ-रात के अंधेरे में, लाखों चांद चमक रहे हैं। मैं उन्हें देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं, लेकिन मेरी दृष्टि कमजोर है।
भली भई जू गुर मिल्या, नहीं तर होती हाँणि।
दीपक दिष्टि पतंग ज्यूँ, पड़ता पूरी जाँणि॥19॥
अर्थ-गुरु मिलना बहुत बड़ी किस्मत की बात है। यदि मुझे गुरु नहीं मिलते, तो मैं भटक जाता।गुरु ज्ञान का दीपक है, जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। जैसे दीपक के प्रकाश से पतंगे आकर्षित होते हैं, वैसे ही गुरु के ज्ञान से मनुष्य आकर्षित होता है।
माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत।
कहै कबीर गुर ग्यान थैं, एक आध उबरंत॥20॥
अर्थ-मनुष्य माया के दीपक के समान है, जो भ्रम में इधर-उधर भटकता रहता है। वह भौतिक सुखों को ही जीवन का सार समझता है और उनमें डूबा रहता है।
लेकिन गुरु का ज्ञान मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त कर सकता है। गुरु उसे सच्चे सुख का मार्ग दिखाता है और उसे जीवन का वास्तविक अर्थ समझाता है।
सतगुर बपुरा क्या करै, जे सिषही माँहै चूक।
भावै त्यूँ प्रमोधि ले, ज्यूँ वंसि बजाई फूक॥21॥
अर्थ- यह कविता सतगुरु और शिष्य के बीच संबंध का वर्णन करती है। कवि कहता है कि यदि शिष्य में ही कोई त्रुटि है, तो सतगुरु क्या कर सकता है? सतगुरु उसे ज्ञान और मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन यदि शिष्य उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे कोई लाभ नहीं होगा।
संसै खाया सकल जुग, संसा किनहुँ न खद्ध।
जे बेधे गुर अष्षिरां, तिनि संसा चुणि चुणि खद्ध॥22॥
अर्थ-यह कविता संसार की क्षणभंगुरता और गुरु के महत्व का वर्णन करती है। कवि कहता है कि संसार ने सभी युगों को खा लिया है, इसका मतलब है कि संसार हमेशा बदलता रहता है और कुछ भी स्थायी नहीं है।
लेकिन जो गुरु की आंखों से देखते हैं, वे संसार का चुनाव करके खाते हैं। इसका मतलब है कि जो गुरु के ज्ञान को ग्रहण करते हैं, वे संसार के मोह में नहीं डूबते और केवल उन चीजों को ग्रहण करते हैं जो उनके लिए आवश्यक हैं।
चेतनि चौकी बैसि करि, सतगुर दीन्हाँ धीर।
निरभै होइ निसंक भजि, केवल कहै कबीर॥23॥
अर्थ- कबीर जी कहते हैं कि हमें आत्म-चेतना में बैठकर ध्यान लगाना चाहिए, सतगुरु की शरण में जाकर उनसे धीरज प्राप्त करना चाहिए, और भय को दूर करके निरंतर भजन करना चाहिए। इस श्लोक में भक्ति और आत्म-जागरूकता की महत्वपूर्ण बातें हैं।
सतगुर मिल्या त का भयां, जे मनि पाड़ी भोल।
पासि बिनंठा कप्पड़ा, क्या करै बिचारी चोल॥24॥
अर्थ- इस दोहे में कबीर जी कह रहे हैं कि सतगुरु के साक्षात्कार से भक्त के मन में निर्मलता और भोलापन आ जाता है। उन्हें भय की कोई अवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनका आत्मा गुरु के प्रकाश में एकाग्र हो जाता है। इसी तरह से, जैसे कपड़ा अपने बाँधने की आवश्यकता खो देता है जब वह किसी और के पास होता है, वैसे ही भक्त को सतगुरु के दर्शन के बाद अपने आप की महत्ता का अहसास होता है।
बूड़े थे परि ऊबरे, गुर की लहरि चमंकि।
भेरा देख्या जरजरा, (तब) ऊतरि पड़े फरंकि॥25॥
अर्थ- इस दोहे में, कबीर जी यह कह रहे हैं कि गुरु की प्रेरणा और उनकी शिक्षा से बूढ़े और अशिक्षित व्यक्ति भी परिवर्तित हो सकते हैं। गुरु की शिक्षा से समझ में आता है कि वास्तविकता क्या है और कैसे जीना चाहिए। भेरे की उसकी जर्जरता देखकर उसने गुरु की ओर रुख किया, इसका अर्थ है कि उसने गुरु के उपदेशों को स्वीकार किया और उनका पालन किया।
कबीर सब जग यों भ्रम्या फिरै ज्यूँ रामे का रोज।
सतगुर थैं सोधी भई, तब पाया हरि का षोज॥27॥
अर्थ- कबीर कहते हैं कि सभी लोग इस प्रकार दिन-रात राम की तलाश में भटकते रहते हैं। परंतु जब मैंने सतगुरु की खोज की, तो मुझे हरि का दर्शन हुआ।”
यह दोहा कबीर जी के द्वारा कही गई एक अद्भुत बात है। इसमें वे बता रहे हैं कि बहुत से लोग अपने जीवन में भगवान की तलाश में भटकते रहते हैं, लेकिन सतगुरु के संदेशों और मार्गदर्शन के बाद ही वे भगवान की साक्षात्कार की प्राप्ति करते हैं।
गुरु गोविन्द तौ एक है, दूजा यह आकार।
आपा मेट जीवत मरै, तो पावै करतार॥26॥
अर्थ-“गुरु और भगवान एक ही हैं, यह दोषरूपी आकार अलग है। जब जीवनी मिट जाती है, तो वही परमात्मा प्राप्त होता है।”
यह दोहा दिखाता है कि गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है। गुरु को समर्पित और उनके मार्गदर्शन में विश्वास रखने से ही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यह दोहा भक्ति मार्ग को सार्थक बनाने के लिए महत्वपूर्ण संदेश प्रदान करता है।
कबीर सतगुर नाँ मिल्या, रही अधूरी सीप।
स्वांग जती का पहरि करि, घरि घरि माँगै भीष॥27॥
अर्थ- कबीर कहते हैं कि मैंने सतगुरु को नहीं पा लिया, और इसलिए मेरी जीवन-यात्रा अधूरी रह गई। मैंने अपनी सारी ऊर्जा और समय का व्यर्थ कर दिया, घर-घर भिख मांगता रहा।”
इस दोहे में कबीर जी व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से अपनी अनगिनत अधिकारियों को साझा करते हैं। उनका संदेश है कि अगर हम सतगुरु का साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं, तो हमारा जीवन अधूरा रह जाता है और हम अपने आत्मिक आनंद को नहीं पा सकते। इसलिए, समय का सही उपयोग करके सतगुरु के प्रति आदर और श्रद्धा रखना आवश्यक है।
कबीर सतगुर ना मिल्या, सुणी अधूरी सीष।
मुँड मुँडावै मुकति कूँ, चालि न सकई वीष॥29॥
अर्थ-“कबीर कहते हैं कि मुझे सतगुरु का दर्शन नहीं मिला, इसलिए मेरी जीवन-यात्रा अधूरी है। मुक्ति का अभिप्राय चरणों को प्राप्त करने से है, लेकिन मुझे वह समर्थ नहीं हो पाई।”
सतगुर साँचा सूरिवाँ, तातै लोहिं लुहार।
कसणो दे कंचन किया, ताई लिया ततसार॥28॥
अर्थ- इस दोहे में कबीर जी कह रहे हैं कि सतगुरु की शिक्षा अत्यंत मूल्यवान है, जैसे कि सोना लोहार के लिए महत्वपूर्ण होता है। उनका यह कहना है कि हमें सतगुरु की शिक्षा को अपनाना चाहिए, उसे अपनाकर ही हम अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं।
थापणि पाई थिति भई, सतगुर दीन्हीं धीर।
कबीर हीरा बणजिया, मानसरोवर तीर॥29॥
अर्थ- इस दोहे में, कबीर जी कह रहे हैं कि जब उन्हें उनके गुरु ने आदर्श और मार्गदर्शन दिया, तो उन्होंने अपने जीवन को सही दिशा में स्थापित किया। उनके अनुसार, उन्होंने समाज में महत्वपूर्ण अंश को निर्मित किया, जिसे उन्होंने एक हीरे के रूप में उत्तरण किया है। इस दोहे में, कबीर जी अपने गुरु की महिमा का गान करते हैं, जिन्होंने उन्हें उनके सार्वभौमिक स्वरूप को पहचानने में मदद की।
कबीर हीरा बणजिया, हिरदे उकठी खाणि।
पारब्रह्म क्रिपा करी सतगुर भये सुजाँण॥
अर्थ- इस दोहे में, कबीर जी अपने भक्ति मार्ग की यात्रा का वर्णन करते हैं। उन्होंने कहा है कि उनके हृदय की गहना, अर्थात उनका आत्मा, अब उन्हें मिल गया है। वे पारब्रह्म की कृपा से सतगुरु के माध्यम से सत्य को पहचान लिया है। इस दोहे में भक्ति और आत्मज्ञान की महत्वपूर्ण बातें हैं।
निहचल निधि मिलाइ तत, सतगुर साहस धीर।
निपजी मैं साझी घणाँ, बांटै नहीं कबीर॥30॥
अर्थ-“निहचल निधि को प्राप्त करने के लिए सतगुरु के साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। मैंने साझा की धन्य समाज के साथ, लेकिन मैंने इसे बांटने का नहीं किया, कबीर कहते हैं।”
अर्थ- इस दोहे में, कबीर जी कह रहे हैं कि सतगुरु के माध्यम से अचल धन को प्राप्त करने के लिए विशेष धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। वे यह भी कह रहे हैं कि वे अपने साझा किए गए धन को दूसरों के साथ साझा कर दिया है, लेकिन उन्होंने इसे बांटने का नहीं किया। यह दोहा नेतृत्व, साहस, और सामाजिक न्याय के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रकट करता है।
चौपड़ि माँडी चौहटै, अरध उरध बाजार।
कहै कबीरा राम जन, खेलौ संत विचार॥31॥
पासा पकड़ा प्रेम का, सारी किया सरीर।
सतगुर दावा बताइया, खेलै दास कबीर॥32॥
अर्थ- इस दोहे में, कबीर जी विश्वास की महत्ता को व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे प्रेम के पासे को पकड़ लिया है, और सम्पूर्ण अपने शरीर का उपयोग किया है ताकि इसे महसूस कर सकें। उन्होंने अपने गुरु से इस सच्चाई को सिखा और इसमें खेला, यानी उसका अनुभव किया। इस दोहे में, प्रेम की अनुभूति को उन्होंने उत्कृष्ट रूप से व्यक्त किया है और गुरु के मार्गदर्शन की महत्ता को भी स्पष्ट किया है।
सतगुर हम सूँ रीझि करि, एक कह्या प्रसंग।
बरस्या बादल प्रेम का भीजि गया अब अंग॥33॥
अर्थ- सतगुरु ने मुझे एक रीति में संधि करा दी, और एक कहानी का प्रसंग सुनाया। प्रेम के बादल बरसे और अब मेरे शरीर को भीगा दिया।”
इस दोहे में, कबीर जी अपने गुरु की महत्ता को व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गुरु की कृपा से उनकी आत्मिक संधि हो गई है और वे एक सत्य कहानी सुनकर सीख गए हैं। उनकी भक्ति की भावना अब उनके अंतर्मन को भीगा दी गई है, जैसे कि बादलों को प्रेम की वर्षा के बाद भूमि को भिगोते हैं।
कबीर बादल प्रेम का, हम परि बरष्या आइ।
अंतरि भीगी आत्माँ हरी भई बनराइ॥34॥
अर्थ- इस दोहे में, कबीर जी व्यक्त कर रहे हैं कि प्रेम का बादल आया है, यानी प्रेम की विशेषता या भावना की वर्षा हुई है। उनके अनुसार, यह प्रेम उनके भीतर के आत्मा को भिगो देता है और उसे हरियाली का रूप धारण करने में सहायक होता है। यहाँ प्रेम की विशेषता या भावना को बादल के रूप में दिखाया गया है, जो आत्मिक और आध्यात्मिक उत्थान को संकेत करता है।
पूरे सूँ परचा भया, सब दुख मेल्या दूरि।
निर्मल कीन्हीं आत्माँ ताथैं सदा हजूरि॥35॥
अर्थ- इस दोहे में, कबीर जी आत्म-समर्पण की महत्ता को व्यक्त कर रहे हैं। जब हम सम्पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आत्मा को परमात्मा के समर्पित करते हैं, तो सभी दुःखों का नाश हो जाता है और हमें सच्चे आत्मिक संबल की प्राप्ति होती है। इस रूप में, परमात्मा हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमें निरंतर गाइड करते हैं।
साखी – बिरह कौ अंग
रात्यूँ रूँनी बिरहनीं, ज्यूँ बंचौ कूँ कुंज।
कबीर अंतर प्रजल्या, प्रगट्या बिरहा पुंज॥1॥
अर्थ- जैसे रात को ही रोने वाली बिरहा समय में अंधेरे के रूप में बादलों में चुपचाप छिप जाती है, वैसे ही कबीर जी अपने आंतरिक विचारों को अंधकार से प्रकाश में परिणत करते हैं, जिससे उनकी बिरहा की पीड़ा प्रकट होती है।”
इस दोहे में, कबीर जी अपनी आत्मा की भावनाओं की व्याख्या कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जैसे रात के अंधेरे में बिरहा समय के अंधेरे में छिप जाती है, वैसे ही उनके आंतरिक भावनाओं का प्रकट होना उनके अंतर मन के अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। इस दोहे में, कबीर जी आत्मा के आंतरिक प्रकट होने की महत्वपूर्णता को बता रहे हैं।
अबंर कुँजाँ कुरलियाँ, गरिज भरे सब ताल।
जिनि थे गोविंद बीछुटे, तिनके कौण हवाल॥2॥
इस दोहे में, कबीर जी संसार की भगवान की असलीता को व्यक्त कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जैसे बादल आये हैं और पक्षियाँ चहक रही हैं, सभी तालों में गर्जन हो रही है, वैसे ही भगवान के साथ जुड़े हुए व्यक्ति कौन हैं, उनका कौन है ध्यान। यह दोहा भगवान की खोज को और उनके साथ जुड़ने की महत्वपूर्णता को उजागर करता है।
चकवी बिछुटी रैणि की, आइ मिली परभाति।
जे जन बिछुटे राम सूँ, ते दिन मिले न राति॥3॥
इस दोहे में, कबीर जी संसार में भगवान के प्रति भक्ति के महत्व को व्यक्त कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति को छोड़ देता है, उसे संसार में संतोष नहीं मिलता, चाहे वह रात हो या दिन। इस दोहे में भगवान के प्रति निष्ठा और उसकी भक्ति के महत्व को प्रकट किया गया है।
बासुरि सुख नाँ रैणि सुख, ना सुख सुपिनै माँहि।
कबीर बिछुट्या राम सूँ ना सुख धूप न छाँह॥4॥
बिरहनि ऊभी पंथ सिरि, पंथी बूझै धाइ।
एक सबद कहि पीव का, कब रे मिलैगे आइ॥5॥
इस दोहे में, कबीर जी अन्याय के खिलाफ खड़े होने और सच्चाई के पथ पर चलने की महत्वपूर्णता को व्यक्त कर रहे हैं। उनके अनुसार, सच्चे मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति कठिनाईयों का सामना करते हैं, लेकिन वे धारणा कर लेते हैं कि सही दिशा में चलना ही सबसे महत्वपूर्ण है। वे प्रश्न करते हैं कि कब हमें सच्चाई का अनुभव होगा?
बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारी राम।
जिव तरसै तुझ मिलन कूँ, मनि नाहीं विश्राम॥6॥
इस दोहे का हिंदी में अनुवाद किया गया है। इसमें कबीर जी भगवान के इच्छुक होने का अर्थ कर रहे हैं और उन्हें अपने साथ मिलने के लिए बेहद बेताबी से प्रतीक्षा है। यह दोहा उनकी भगवान के आवश्यकता और उनके दर्शन के प्रती प्रतीक्षा को व्यक्त करता है। यह भावना आत्मा की अधिकांश खोज का परिणाम होता है, जब उसे भगवान के प्रति प्रेम और आकर्षण होता है।
बिरहिन ऊठै भी पड़े, दरसन कारनि राम।
मूवाँ पीछे देहुगे, सो दरसन किहिं काम॥7॥
इस दोहे में, कबीर जी बता रहे हैं कि जब भक्त अपने भगवान के दर्शन की इच्छा से उठते हैं, तो उनकी यात्रा की पराकाष्ठा सफल होती है। वे उस दर्शन की अवश्यकता को इतनी महत्वपूर्ण मानते हैं कि वे उसकी प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए, उन्हें दर्शन की कोई चीज बड़ी नहीं होती, और वे उसे प्राप्त करने के लिए सभी कष्टों को सहन करते हैं।
मूवाँ पीछै जिनि मिलै, कहै कबीरा राम।
पाथर घाटा लोह सब, (तब) पारस कौंणे काम॥8॥
इस दोहे में, कबीर जी भगवान के आस्थान को बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के पास जाता है, वही सच्चा भगवान है। सारे पत्थर, घाटा और लोहे तो हैं, लेकिन कौन सा पारस (सोने की खोज) सच्चे मुक्ति और आत्मा के लिए महत्वपूर्ण है, यह विचार कबीर जी व्यक्त कर रहे हैं।
अंदेसड़ा न भाजिसी, संदेसो कहियाँ।
कै हरि आयां भाजिसी, कै हरि ही पासि गयां॥9॥
इस दोहे में, कबीर जी व्यक्ति को उसकी अस्थिरता और मायावी विचारों के बारे में चेतावनी देते हैं। उनके अनुसार, जब हम अपनी अस्थिरता को समझते हैं, तब हम वास्तविक सत्य को समझने के लिए तत्परता प्राप्त करते हैं। भगवान किसी के पास आते हैं और किसी को वही दूर चला जाते हैं, इसलिए हमें स्थिरता और सत्य की खोज में लगे रहना चाहिए।
आइ न सकौ तुझ पै, सकूँ न तूझ बुझाइ।
जियरा यौही लेहुगे, बिरह तपाइ तपाइ॥10॥
इस दोहे में, कबीर जी भगवान की खोज में अपने भक्तों की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मनुष्य अपनी परमात्मा को समझने में असमर्थ है, मनुष्य जितना भगवान को चाहता है, उतना ही उसकी बिरहा का तप भी बढ़ जाता है
यहु तन जालौं मसि करूँ, ज्यूँ धूवाँ जाइ सरग्गि।
मति वै राम दया, करै, बरसि बुझावै अग्गि॥11॥
इस दोहे में, कबीर जी भगवान की प्रेम को व्यक्त करते हैं और उनकी उपासना का तरीका बताते हैं। वे कहते हैं कि उनके शरीर को कसेंगे और अपने मन को इन्द्रियों के अवलोकन से पार करेंगे। जब हम भगवान के प्रेम को बुद्धि से पहचानते हैं, तो हमारी आग सारी बुझ जाती है, अर्थात् हमारा मन पवित्रता की ओर बढ़ता है।
कबीर पीर पिरावनीं, पंजर पीड़ न जाइ।
एक ज पीड़ परीति की, रही कलेजा छाइ॥13॥
इस दोहे में, कबीर जी मानवता के अद्वितीय गुणों को उजागर करते हैं। उन्हें बताया जाता है कि जो व्यक्ति अपने आस-पास के लोगों के दुःखों को समझता है और उनकी मदद करता है, उसकी आत्मा कभी पीड़ित नहीं होती है। इससे वह सच्चे प्रेम का अनुभव करता है और उसकी आत्मा हमेशा शांत और तृप्त रहती है।
चोट सताड़ी बिरह की, सब तन जर जर होइ।
मारणहारा जाँणिहै, कै जिहिं लागी सोइ॥14॥
इस दोहे में, कबीर जी व्यक्ति के भावनात्मक दुःख को व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा है कि बिरहा का दुःख बहुत तेज़ होता है और इससे शरीर में जलन की भावना होती है। उन्होंने भी यह कहा है कि सिर्फ वही व्यक्ति जानता है कि किसे कैसा प्रभाव डाला गया है जो इस दुःख को अनुभव कर रहा है।
कर कमाण सर साँधि करि, खैचि जू मार्या माँहि।
भीतरि भिद्या सुमार ह्नै जीवै कि जीवै नाँहि॥15॥
इस दोहे में, कबीर जी व्यक्ति को जीवन के संघर्षों और परीक्षणों के सामना करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं और हमें सामना करना पड़ता है, तो हमारी आत्मा में एक गहरी दरार पैदा होती है। क्या हम उस दरार को जीवित रख सकते हैं या नहीं, यह हमारे व्यक्तित्व की गहरी परीक्षा होती है।
जबहूँ मार्या खैंचि करि, तब मैं पाई जाँणि।
लांगी चोट मरम्म की, गई कलेजा जाँणि॥16॥
इस दोहे में, कबीर दास जी कहते हैं कि जब उन्हें तीर से घायल किया गया तो उन्हें सच्चाई का अनुभव हुआ। यहाँ ‘तीर’ का अर्थ विवेक या दुखदाई अनुभव है। ‘लांगी चोट’ का अर्थ है महान चोट, जिससे ‘मरम्म’, यानी अंतरात्मा को चोट पहुंची है, और ‘कलेजा’ का अर्थ हृदय है। इस दोहे में कबीर दास जी अपने अनुभवों के माध्यम से बताते हैं कि असली सच्चाई को समझने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करना आवश्यक है।
जिहि सर मारी काल्हि सो सर मेरे मन बस्या।
तिहि सरि अजहूँ मारि, सर बिन सच पाऊँ नहीं॥17॥
इस दोहे में, कबीर दास जी कहते हैं कि जो सिर को मारता है, वही सिर मेरे मन में बसता है। ‘काल्हि’ या ‘कान’ का अर्थ यहाँ समझाया जा सकता है कि जो व्यक्ति विवेक के विरुद्ध कार्य करता है, उसका मन में बसता है। इसका मतलब है कि अमानवीय कार्य करने वाले का मन उसी के साथ रहता है और वह अमानवीयता में डूबा रहता है। दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि जिस सिर को मारा जाता है, उस सिर के बिना मैं सच्चाई को पाने के लिए सक्षम नहीं हूं। यहाँ ‘सिर’ का अर्थ विवेक है, जो व्यक्ति के आत्मचिंतन और सत्य के प्रति जागरूकता को प्रतिनिधित्ता करता है। इस पंक्ति में यह बताया जा रहा है कि सत्य को पहचानने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है।
बिरह भुवंगम तन बसै, मंत्रा न लागै कोइ।
राम बियोगी ना जिवै, जिवै त बीरा होइ॥18॥
इस दोहे में, कबीर दास जी कह रहे हैं कि जब विरह या अलगाव का दुख व्यक्ति के शरीर में बस जाता है, तो कोई भी मंत्र उसे ठीक नहीं कर सकता है। ‘राम’ यहाँ भगवान की उपस्थिति को संदर्भित करता है। यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में जीता है, वह सच्चे वीर के समान होता है।
बिरह भुवंगम पैसि करि, किया कलेजै घाव।
साधू अंग न मोड़ही, ज्यूँ भावै त्यूँ खाव॥19॥
इस दोहे में, कबीर दास जी कह रहे हैं कि विरह का दुख व्यक्ति के हृदय को बहुत गहरा घाव पहुंचाता है। ‘साधू अंग न मोड़ही’ का अर्थ है कि वे संत अपने आप को विचलित नहीं करते हैं, चाहे उन्हें कितना ही दुख हो। इसका अर्थ है कि वे हमेशा उदार और सहानुभूति रहते हैं और अपनी आत्मा की ऊँचाई को बनाए रखते हैं। वे अपने भाव के अनुसार जीते हैं और खाते हैं।
सब रग तंत रबाब तन, बिरह बजावै नित्त।
और न कोई सुणि सकै, कै साई के चित्त॥20॥
इस दोहे में, कबीर दास जी यह कह रहे हैं कि हमारे शरीर के सभी रग-रस्ते और मानसिक तंत्रे भगवान की याद में संगीत की भाँति ध्वनित होते हैं। विरह के दुख सदैव हमारे मन में वाजते रहते हैं। किसी को भी यह ध्वनि सुनने में समर्थ नहीं होती है, क्योंकि विरह का दुख केवल उस व्यक्ति के मन में ही होता है जिसका मन भगवान की ओर लगा हुआ हो
बिरहा बिरहा जिनि कहौ, बिरहा है सुलितान।
जिह घटि बिरह न संचरै, सो घट सदा मसान॥21॥
इस दोहे में, कबीर दास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ‘बिरहा’ की बात करता है, वही ‘बिरहा’ का सिकंदर है। ‘बिरहा’ यहाँ अलगाव या दुःख को संदर्भित करता है। जो किसी व्यक्ति का मन ‘बिरहा’ के दुःख से बाहर नहीं निकलता, वही मन सदा ही मृत्यु के समान होता है।
अंषड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारि निहारि।
जीभड़ियाँ छाला पड़्या, राम पुकारि पुकारि॥22॥
इस दोहे में, कबीर दास जी द्वारा कहा गया है कि उन्हें अंशदारी और विचार करते हुए सभी पथ का अंश यथार्थतः जानने का अनुभव हो रहा है। उनकी जीभड़ी में भी राम के नाम की ध्वनि बनी हुई है, जो लगातार पुकार रही है। इस दोहे में राम के नाम के महत्व को उजागर किया गया है।
इस तन का दीवा करौं, बाती मेल्यूँ जीव।
लोही सींचौ तेल ज्यूँ, कब मुख देखौं पीव॥23॥
इस दोहे में, कबीर दास जी कह रहे हैं कि वह अपने शरीर को एक दीया की भाँति बनाना चाहते हैं और उसे इस जगह में मिलने वाले दिव्य जीवन की बातियों से जलाना चाहते हैं। वे तेल के समान अपने मुख को सींचना चाहते हैं, ताकि उन्हें दिव्य अनुभव हों। यहाँ ‘तेल’ का उपयोग आत्मा की शुद्धि और प्राप्ति के लिए किया गया है।
नैंना नीझर लाइया, रहट बहै निस जाम।
पपीहा ज्यूँ पिव पिव करौं, कबरू मिलहुगे राम॥24॥
इस दोहे में, कबीर दास जी कह रहे हैं कि जैसे जैसे पपीहा पानी पीता है, उसी तरह वह भी भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल होता है। ‘नैंना नीझर लाइया’ का अर्थ है कि अपनी आँखों को बंद करके, अंतर्मन से परमात्मा की अनुभूति करता है। उन्हें यहाँ प्रेरित किया जाता है कि उनकी श्रद्धा और आसक्ति की भावना के समान पपीहा की तरह हो, ताकि वह भगवान को मिल सके।
अंषड़िया प्रेम कसाइयाँ, लोग जाँणे दुखड़ियाँ।
साँई अपणैं कारणै, रोइ रोइ रतड़िया॥25॥
इस दोहे में, कबीर दास जी कह रहे हैं कि अधिकांश लोग प्रेम को एक धोखे की तरह देखते हैं, और उन्हें इससे दुःख होता है। वे कहते हैं कि भक्त भगवान के प्रति अपने प्रेम को अपनी आत्मविश्वास में निर्मित करता है, और फिर भगवान की प्राप्ति के लिए रोता रहता है।
सोई आँसू सजणाँ, सोई लोक बिड़ाँहि।
जे लोइण लोंहीं चुवै, तौ जाँणों हेत हियाँहि॥26॥
इस दोहे में, कबीर दास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक व्यक्ति के आँसू अपने प्रियजनों को चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार वे ही लोग उसी के विरुद्ध बिदा करते हैं। उन्हें यहाँ बताया जाता है कि जैसे कि लोहे को जिस चीज़ का स्पर्श होता है, वह उसका उसके गुणों के अनुसार उत्तर देता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के मन की भावनाओं को उसका हृदय बता देता है।
कबीर हसणाँ दूरि करि, करि रोवण सौं चित्त।
बिन रोयाँ क्यूँ पाइये, प्रेम पियारा मित्त॥27॥
इस दोहे में, कबीर दास जी कह रहे हैं कि वे हँसने और रोने को बराबर मानते हैं, और दोनों का अपने मन में स्थान है। उनके अनुसार, प्रेम और प्रियतम से बिना रोये, मनुष्य क्यों पाए? अर्थात्, बिना प्रेम के, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, व्यक्ति क्यों पाए?
जौ रोऊँ तो बल घटे, हँसौं तो राम रिसाइ।
मनही माँहि बिसूरणाँ, ज्यूँ घुंण काठहि खाइ॥28॥
इस दोहे में, कबीर दास जी कह रहे हैं कि अगर वह रोएँ तो उनका बल कम हो जाता है, लेकिन अगर हँसें तो उन्हें राम का आनंद मिलता है। वे कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन की चापलूसी से निपटना चाहिए, जैसे कि खाद्य को लट्ठा काटकर काम में लाया जाता है।
हंसि हंसि कंत न पाइए, जिनि पाया तिनि रोइ।
जो हाँसेही हरि मिलै, तो नहीं दुहागनि कोइ॥29॥
इस दोहे में, कबीर दास जी कह रहे हैं कि वह लोग जो हंसते हंसते कामना से अपने लक्ष्य नहीं पाते, उन्हें वही रोते हुए पाया जाता है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति हंसते हंसते ही भगवान को पा लेता है, उसके लिए कोई भी दुखी नहीं हो सकता।
हाँसी खेलौ हरि मिलै, तौ कौण सहे षरसान।
काम क्रोध त्रिष्णाँ तजै, ताहि मिलैं भगवान॥30॥
इस दोहे में, कबीर दास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हंसते हंसते और खेलते हुए भगवान को पा लेता है, उसके लिए किसी प्रकार का दुःख भी सहनीय नहीं होता। उन्हें बताया जाता है कि व्यक्ति को अपनी कामनाओं, क्रोध और तृष्णाओं को त्यागना चाहिए, क्योंकि उसी से भगवान का दर्शन होता है।
पूत पियारो पिता कौं, गौंहनि लागा धाइ।
लोभ मिठाई हाथ दे, आपण गया भुलाइ॥31॥
इस दोहे में, कबीर दास जी कह रहे हैं कि पुत्र अपने पिता के प्रति अत्यंत प्रेम करता है, लेकिन जब वह लोभी होता है और अन्यायपूर्ण भावनाओं के बल पर अपने पिता के साथ विश्वासघात करता है, तो वह खुद को भूल जाता है।
डारि खाँड़ पटकि करि, अंतरि रोस उपाइ।
रोवत रोवत मिलि गया, पिता पियारे जाइ॥32॥
इस दोहे में, कबीर दास जी कह रहे हैं कि जब हम अपने अन्तर में भ्रमित और उदास होते हैं, तो हमें अपने परमात्मा का अनुभव होता है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति रोते-रोते अपने परमात्मा को पा लेता है, वह सच्चे पिता के पास जाता है।
टिप्पणी: ख-में इसके अनंतर यह दोहा है-
मो चित तिलाँ न बीसरौ, तुम्ह हरि दूरि थंयाह।
इहि अंगि औलू भाइ जिसी, जदि तदि तुम्ह म्यलियांह॥
इस पद में, कबीर दास ईश्वर को संबोधित करते हुए व्यक्त कर रहे हैं कि वह एक क्षण के लिए भी ईश्वरीय उपस्थिति को कभी नहीं भूलेंगे या उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे। भगवान को दूर महसूस करने के बावजूद, कबीर आश्वस्त करते हैं कि भगवान कभी दूर नहीं हैं। यहां, कबीर ने रूपक रूप से खुद की तुलना एक उल्लू से की है, और सुझाव दिया है कि जिस तरह उल्लू दिन की रोशनी में नहीं देख सकता है, उसी तरह, वह कभी-कभी आध्यात्मिक रूप से अंधा महसूस करता है, लेकिन फिर भी, वह परमात्मा से जुड़ा हुआ है।
नैना अंतरि आचरूँ, निस दिन निरषौं तोहि।
कब हरि दरसन देहुगे सो दिन आवै मोंहि॥33॥
इस पद में कबीर दास ने ईश्वर के दर्शन की अपनी लालसा व्यक्त की है। उनका कहना है कि वह अपनी आंतरिक दृष्टि को लगातार ईश्वर पर केंद्रित रखते हैं और वह दिन-रात उस क्षण की प्रतीक्षा में बेचैन रहते हैं जब अंततः उन्हें ईश्वरीय उपस्थिति को देखने का सौभाग्यशाली अवसर मिलेगा।
कबीर देखत दिन गया, निस भी देखत जाइ।
बिरहणि पीव पावे नहीं, जियरा तलपै भाइ॥34॥
इस पद में कबीर अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना दिन बीतने पर विचार करते हैं। वह गुज़रते दिनों की तुलना परमात्मा की ओर निरंतर यात्रा से करते हैं। इस चल रही यात्रा के बावजूद, वह परमात्मा के लिए अलगाव और लालसा की गहरी भावना महसूस करता है, इसकी तुलना एक प्यासे व्यक्ति से की जाती है जो पानी खोजने में असमर्थ है, लगातार तरस रहा है और सांत्वना की तलाश कर रहा है।
कै बिरहनि कूं मींच दे, कै आपा दिखलाइ।
आठ पहर का दाझणां, मोपै सह्या न जाइ॥35॥
इस पद में, कबीर अलगाव के निवारण और ईश्वर के प्रत्यक्ष रहस्योद्घाटन की इच्छा रखते हैं। वह अलगाव की पीड़ा से राहत पाने के लिए दिव्य उपस्थिति की अपनी इच्छा व्यक्त करता है। लंबे समय तक अलगाव के दर्द को सहने के बावजूद, उसे कोई राहत या आराम नहीं मिलता है, इस बात पर जोर देते हुए कि उसकी लालसा की तीव्रता बरकरार है।
बिरहणि थी तो क्यूँ रही, जली न पीव के नालि।
रहु रहु मुगध गहेलड़ी, प्रेम न लाजूँ मारि॥36॥
इस पद में, कबीर सवाल करते हैं कि अलगाव की पीड़ा का अनुभव करने के बावजूद, परमात्मा का साधक, कुएं के पानी से अपनी प्यास बुझाने के समान, दिव्य प्रेम में डूबकर सांत्वना क्यों नहीं ढूंढता है। वह इस स्थिति की तुलना एक मूर्ख हिरण से करता है जो भागने का कोई प्रयास किए बिना गहरे गड्ढे में फंसा रहता है। इसी प्रकार, दिव्य प्रेम की भावना से रहित साधक अज्ञानी बना रहता है और अलगाव की पीड़ा से राहत पाने में असफल रहता है।
हौं बिरहा की लाकड़ी, समझि समझि धूंधाउँ।
छूटि पड़ौं यों बिरह तें, जे सारीही जलि जाउँ॥37॥
इस पद में कबीर ने अलगाव की पीड़ा को लकड़ी के टुकड़े के रूप में रूपक रूप से वर्णित किया है। उनका सुझाव है कि व्यक्ति अक्सर इस दर्द को समझने या उसका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, जैसे अंधेरे में कुछ खोजना। हालाँकि, अलगाव के इस दर्द से वास्तविक मुक्ति तब होती है जब कोई इससे पूरी तरह भस्म हो जाता है, जैसे लकड़ी आग से भस्म हो जाती है। श्लोक का तात्पर्य है कि केवल अलगाव के दर्द को पूरी तरह से अनुभव करने और उसके प्रति समर्पण करने से ही कोई इससे पार पा सकता है।
कबीर तन मन यों जल्या, बिरह अगनि सूँ लागि।
मृतक पीड़ न जाँणई, जाँणैगि यहूँ आगि॥38॥
इस पद में, कबीर ने ईश्वर से अलगाव की तीव्र पीड़ा का वर्णन अपने शरीर और मन को जलाने, अलगाव की आग में जलने के समान किया है। वह लाक्षणिक रूप से इस पीड़ा की तुलना जिंदा जलाए जाने से करता है। कबीर आगे सुझाव देते हैं कि जिन लोगों ने अलगाव की इस पीड़ा का अनुभव नहीं किया है, वे वास्तव में इसे समझ नहीं सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे जो व्यक्ति मरा नहीं है वह मृतक के दर्द को नहीं समझ सकता है। उनका तात्पर्य यह है कि केवल वे ही जो व्यक्तिगत रूप से इस तीव्र लालसा और अलगाव से गुज़रे हैं, वास्तव में इसकी गहराई और तीव्रता को समझ सकते हैं।
बिरह जलाई मैं जलौं, जलती जल हरि जाउँ।
मो देख्याँ जल हरि जलै, संतौं कहीं बुझाउँ॥39॥
इस पद में, कबीर ने ईश्वर से मिलन की अपनी गहरी लालसा व्यक्त की है और इसकी तुलना विरह की जलती आग से की है। वह कहते हैं कि वह स्वयं विरह की इस अग्नि में भस्म हो गए हैं और इस जलन में केवल ईश्वर का सार ही शेष रह जाता है। कबीर इस दिव्य तत्व को हर जगह जलते हुए देखना चाहते हैं, जैसे दिव्य अग्नि को हर चीज में व्याप्त देखना। वह इस समझ को संतों के साथ साझा करना चाहते हैं, जो पूरे अस्तित्व में व्याप्त दिव्य उपस्थिति के बारे में दूसरों को प्रबुद्ध करने की उनकी इच्छा को दर्शाता है।
परबति परबति में फिर्या, नैन गँवाये रोइ।
सो बूटी पाऊँ नहीं, जातें जीवनि होइ॥40॥
इस कविता में, कबीर ने रूपक रूप से ईश्वर की खोज में भटकने को पहाड़ों को पार करने के रूप में वर्णित किया है, जहां व्यक्ति गंतव्य की दृष्टि खो देता है और पीड़ा में रोता है। यह कल्पना आध्यात्मिक खोज में आने वाली कठिनाई और भ्रम का सुझाव देती है। कबीर को अफसोस है कि इतनी भटकने के बावजूद, उन्हें दिव्य सार नहीं मिला है, इसकी तुलना अमरता प्रदान करने वाली जड़ी-बूटी (बूटी) न मिलने से की जाती है, जिसका अर्थ है कि जीवन का असली सार या आध्यात्मिक पूर्ति मायावी बनी हुई है।
फाड़ि फुटोला धज करौं, कामलड़ी पहिराउँ।
जिहि जिहिं भेषा हरि मिलैं, सोइ सोइ भेष कराउँ॥41॥
इस कविता में, कबीर ने ईश्वर की निकटता प्राप्त करने के लिए अपने अहंकार और बाहरी दिखावे को त्यागने की प्रक्रिया का प्रतीकात्मक रूप से वर्णन किया है। वह अहंकार और अभिमान के कपड़े को फाड़ने और कमल के पत्ते की प्रतीक सादगी और विनम्रता से खुद को सजाने का सुझाव देते हैं। कबीर आगे इस बात पर जोर देते हैं कि जैसे-जैसे कोई ईश्वर के साथ मिलन की ओर बढ़ता है, उन्हें वह रूप अपनाना चाहिए जो उनके सामने आने वाले दैवीय गुणों को दर्शाता है, जो आंतरिक परिवर्तन और दैवीय गुणों के साथ संरेखण की आवश्यकता को दर्शाता है।
नैन हमारे जलि गये, छिन छिन लोड़ै तुझ।
नां तूं मिलै न मैं खुसी, ऐसी बेदन मुझ॥42॥
इस पद में, कबीर ने रूपक रूप से यह कहकर ईश्वर से अलग होने की गहरी पीड़ा व्यक्त की है कि उनकी आँखें आँसू बन गई हैं और उनका हृदय ईश्वर के लिए निरंतर पीड़ा महसूस करता है। उसे ऐसा महसूस होता है मानो हर पल ईश्वर की लालसा में व्यतीत हो रहा है, और यह लालसा बढ़ती ही जाती है, जिससे उसे परेशानी और पीड़ा होती है। कबीर आगे अफसोस जताते हुए कहते हैं कि न तो उन्हें खुशी मिलती है और न ही भगवान उनसे मिलने आते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें इतना गहरा दुख होता है।
भेला पाया श्रम सों, भौसागर के माँह।
जो छाँड़ौ तौ डूबिहौ, गहौं त डसिये बाँह॥43॥
इस पद में कबीर गहन आध्यात्मिक संदेश देने के लिए रूपक भाषा का प्रयोग करते हैं। वह जीवन की तुलना कठिनाइयों और चुनौतियों (भवसागर) के विशाल महासागर को पार करने से करता है। रूपक से पता चलता है कि जीवन समुद्र के अशांत पानी में नौकायन करने के समान संघर्षों और प्रयासों (श्रम) से भरा है। कबीर मानव अस्तित्व की दुविधा पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि यदि कोई इन चुनौतियों से बचने की कोशिश करता है, तो वे डूब सकते हैं, लेकिन अगर वे उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं (यानी, सांसारिक गतिविधियों से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं), तो वे भी उनमें भस्म हो जाएंगे। कविता जीवन में संतुलन और वैराग्य खोजने, चुनौतियों से अभिभूत हुए बिना उनका सामना करने के महत्व पर जोर देती है।
बिरह जलाई मैं जलौं, मो बिरहिन कै दूष।
छाँह न बैसों डरपती, मति जलि ऊठे रूष॥46॥
इस पद में, कबीर ने ईश्वर से अलगाव की पीड़ा से ग्रस्त होने की अपनी स्थिति व्यक्त की है। वह रूपक रूप से खुद को अलगाव में आग लगाने के रूप में वर्णित करता है, जिसका अर्थ है कि वह अलगाव के दर्द से घिरा हुआ है। इसके बाद कबीर ने इसकी तुलना उस व्यक्ति की स्थिति से की जो परमात्मा (बिरहिन) से अलग नहीं है, यह सुझाव देते हुए कि वे शुद्ध हैं। वह भय (अलगाव के) की छाया में न बैठने का आग्रह करता है, क्योंकि समझ (मति) प्रज्वलित होने पर मन में आक्रोश (क्रोध या कड़वाहट) पैदा होता है (जल उठे रुष)। यह कविता ईश्वर से अलगाव की गहरी आध्यात्मिक पीड़ा और शांति और स्वीकृति की स्थिति बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डालती है।
रैणा दूर बिछोहिया, रह रे संषम झूरि।
देवलि देवलि धाहड़ी, देखी ऊगै सूरि॥44॥
इस पद में, कबीर ने गहन आध्यात्मिक संदेश देने के लिए रूपकों का प्रयोग किया है। वह रात (रैना) की तुलना साधक को ईश्वर से अलग करने वाली दूरी (दूर) से करता है। इस दूरी के बावजूद, कबीर धैर्यवान और संयमित रहने (राह रे संसंम झूरी) और अधीरता या निराशा से अभिभूत न होने की सलाह देते हैं। इसके बाद उन्होंने अलंकारिक रूप से सुबह होने (देवली देवली धारी) को दैवीय उपस्थिति की अभिव्यक्ति के रूप में वर्णित किया, इसकी तुलना शेर (धाढ़ी) की दहाड़ से की, जिससे पता चलता है कि दैवीय सत्य की प्राप्ति आसन्न है। यह श्लोक आध्यात्मिक यात्रा में धैर्य और दृढ़ता के महत्व को रेखांकित करता है, इस आश्वासन के साथ कि आत्मज्ञान की सुबह अंततः आएगी।
सुखिया सब संसार है, खाये अरु सोवै।
दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवै॥45॥
इस पद में, कबीर सांसारिक सुख की सामान्य स्थिति की तुलना अपनी आध्यात्मिक असंतोष की स्थिति से करते हैं। उनका मानना है कि दुनिया में ज्यादातर लोग संतुष्ट, भौतिक सुखों में लिप्त और शांति से सोते हुए दिखते हैं। हालाँकि, कबीर खुद को दुखी (दुखिया) मानते हैं, क्योंकि वे जागृत हैं और गहरी आध्यात्मिक सच्चाइयों से अवगत हैं। जबकि अन्य लोग अज्ञानता में सोते हैं, कबीर जागते रहते हैं, ईश्वर से अलग होने के दर्द का अनुभव करते हैं और आध्यात्मिक जागृति की लालसा रखते हैं।
साखी – ग्यान बिरह कौ अंग
दीपक पावक आंणिया, तेल भी आंण्या संग।
तीन्यूं मिलि करि जोइया, (तब) उड़ि उड़ि पड़ैं पतंग॥1॥
यह दोहा भारतीय साहित्य का हिस्सा है, जिसे संत कबीर ने रचा है। इस दोहे में कबीर जी कह रहे हैं कि मतलब दीपक की ज्योति को भले ही पावक और तेल के संयोग से उत्पन्न किया जाए, लेकिन यह सिर्फ उसकी ज्योति को प्रकट नहीं कर सकता। वैसे ही जैसे कि पतंग को उड़ने के लिए उसको ऊपर की ओर उड़ने की जरूरत होती है, वैसे ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को ऊँचाईयों की ओर जाना होता है।
मार्या है जे मरेगा, बिन सर थोथी भालि।
पड्या पुकारे ब्रिछ तरि, आजि मरै कै काल्हि॥2॥
यह दोहा भाग्य की अनिवार्यता और जीवन की अवधि की अनिश्चितता को दर्शाता है। यह सुझाव देता है कि मृत्यु सभी को आती है, चाहे उनकी परिस्थिति कुछ भी हो, और यह कब घटित होगी इसकी अप्रत्याशितता पर जोर देता है, इसकी तुलना एक पेड़ के गिरने से होती है जब एक कठफोड़वा उस पर चोंच मारता है।
हिरदा भीतरि दौ बलै, धूंवां प्रगट न होइ।
जाके लागी सो लखे, के जिहि लाई सोइ॥3॥
भले ही आँगन के अंदर दो चाँद हों, अगर रोशनी न हो, तो वह चमक नहीं पाएगा। जो होना तय है, वह होगा, बाकी कुछ नहीं होगा।”
यह दोहा इस बात पर जोर देता है कि केवल क्षमता या संसाधन होना ही पर्याप्त नहीं है; कार्रवाई और परिस्थितियाँ परिणाम प्रकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह नियति की अनिवार्यता और जो होता है उसे स्वीकार करने के महत्व पर जोर देता है।
झल उठा झोली जली, खपरा फूटिम फूटि।
जोगी था सो रमि गया, आसणि रही बिभूत॥4॥
यह दोहा जीवन और भौतिक संपत्ति की क्षणिक प्रकृति को रूपक रूप से चित्रित करता है। थैले को उठाना और गठरी को जलाना सांसारिक आसक्तियों और इच्छाओं की नश्वरता का प्रतीक है। तपस्वी, सांसारिक मोह-माया को त्यागकर, केवल राख छोड़कर, खुशी-खुशी इस दुनिया से चला जाता है। यह वैराग्य की अवधारणा और भौतिक अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति को रेखांकित करता है।
अगनि जू लागि नीर में, कंदू जलिया झारि।
उतर दषिण के पंडिता, रहे विचारि बिचारि॥5॥
यह दोहा पानी में जलती हुई आग और अपने ही रस में उबलती लौकी की एक विरोधाभासी छवि प्रस्तुत करता है, उन स्थितियों को दर्शाता है जहां कुछ असंभव प्रतीत होता है। यह जीवन के विरोधाभासों और रहस्यों का प्रतीक है। दूसरी पंक्ति में उल्लिखित दक्षिण के विद्वान उन लोगों को संदर्भित कर सकते हैं जो गहन चिंतन और प्रतिबिंब के माध्यम से ज्ञान और समझ चाहते हैं।
दौं लागी साइर जल्या, पंषी बैठे आइ।
दाधी देह न पालवै सतगुर गया लगाइ॥6॥
यह दोहा गहन आध्यात्मिक सच्चाइयों को व्यक्त करने के लिए रूपक भाषा का उपयोग करता है। घास के ढेर में आग लगना और उस पर बैठे पक्षी सांसारिक परेशानियों और विकर्षणों का प्रतीक हैं। दूध का फटना किसी शुद्ध चीज़ को एक अलग रूप में बदलने का प्रतिनिधित्व करता है। आध्यात्मिक शिक्षाओं के संदर्भ में, ये घटनाएँ आत्मज्ञान के मार्ग पर आने वाली चुनौतियों और परिवर्तनों को दर्शाती हैं। सच्चे गुरु द्वारा छाप छोड़ने का उल्लेख किसी के जीवन पर आध्यात्मिक मार्गदर्शन और ज्ञानोदय के स्थायी प्रभाव का सुझाव देता है।
गुर दाधा चेल्या जल्या, बिरहा लागी आगि।
तिणका बपुड़ा ऊबर्या, गलि पूरे के लागि॥7॥
यह दोहा अपने गुरु की झोपड़ी जलने पर शिष्यों द्वारा अनुभव की गई परेशानी और उथल-पुथल का वर्णन करने के लिए कल्पना का उपयोग करता है। जलती हुई झोपड़ी मार्गदर्शन और ज्ञान की हानि का प्रतीक है। टिंडर द्वारा दर्शाए गए शिष्यों ने आग पकड़ ली, जिससे पता चलता है कि वे नुकसान से गहराई से प्रभावित हैं। धुएँ से भरी गली भ्रम और अनिश्चितता का प्रतीक है। कुल मिलाकर, कविता आध्यात्मिक मार्गदर्शन खोने के गहरे प्रभाव और शिष्यों द्वारा महसूस किए गए परिणामी भटकाव पर जोर देती है।
आहेड़ी दौ लाइया, मृग पुकारै रोइ।
जा बन में क्रीला करी, दाझत है बन सोइ॥8॥
यह दोहा सांसारिक प्रलोभनों और जाल में फंसने के परिणामों को दर्शाने के लिए एक शिकारी के जाल बिछाने और एक जानवर के पकड़े जाने के रूपक का उपयोग करता है। फंसे हुए जानवर का रोना पीड़ा और अफसोस का प्रतीक है। इसी तरह, जब कोई पक्षी जंगल में फंस जाता है, तो उसे खतरे का एहसास होता है और जंगल में प्रवेश करने के अपने फैसले पर पछतावा होता है। यह कविता जीवन की चुनौतियों और प्रलोभनों से निपटने में सावधानी और विवेक बरतने के महत्व पर प्रकाश डालती है।
पाणी मांहे प्रजली, भई अप्रबल आगि।
बहती सलिता रहि गई, मेछ रहे जल त्यागि॥9॥
यह दोहा आध्यात्मिक सत्य को व्यक्त करने के लिए रूपक भाषा का उपयोग करता है। पानी का जलना आग के प्रतीक एक बड़ी ताकत के सामने सांसारिक तत्वों की असुरक्षा और शक्तिहीनता को दर्शाता है। इसके विपरीत, बहती हुई नदी अप्रभावित और शांत रहती है, जो सांसारिक उथल-पुथल से लचीलापन और वैराग्य का संकेत देती है। इसी प्रकार, मछली स्वेच्छा से अपना निवास स्थान, पानी, छोड़ देती है, जिसका अर्थ है भौतिक आसक्तियों से वैराग्य। कुल मिलाकर, यह कविता जीवन की चुनौतियों और परिवर्तनों के बीच शांत और अलग रहने के महत्व पर जोर देती है
समंदर लागी आगि, नदियां जलि कोइला भई।
देखि कबीरा जागि, मंछी रूषां चढ़ि गई॥10॥
यह दोहा गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि व्यक्त करने के लिए ज्वलंत कल्पना का उपयोग करता है। समुद्र में आग लगना और नदियाँ कोयले में बदल जाना प्राकृतिक क्रम में होने वाले गहन व्यवधानों और परिवर्तनों का प्रतीक है। कबीर की जागृति इन असाधारण घटनाओं को देखने पर एक अहसास या आत्मज्ञान का सुझाव देती है। क्रोध में आरोही मछली ऐसी असाधारण घटनाओं के कारण होने वाली गड़बड़ी पर प्रतिक्रिया करने वाले प्राणियों का प्रतिनिधित्व कर सकती है, जो उथल-पुथल और परिवर्तन के प्रति सार्वभौमिक प्रतिक्रिया को उजागर करती है। कुल मिलाकर, यह कविता दुनिया की नश्वरता और अप्रत्याशितता और अराजकता के बीच आध्यात्मिक जागृति और समझ की आवश्यकता पर जोर देती है।
बिरहा कहै कबीर कौं तू जनि छाँड़े मोहि।
पारब्रह्म के तेज मैं, तहाँ ले राखौं तोहि॥
इस दोहे में, कबीर ने “बिरहा” को व्यक्त किया है, जिसे परमात्मा के लिए अलगाव या लालसा की भावना के रूप में समझा जा सकता है। कबीर सवाल करते हैं कि कोई व्यक्ति लालसा की इस भावना से क्यों दूर हो जाएगा, क्योंकि इस लालसा के माध्यम से ही कोई ईश्वर से मिलन पा सकता है। वह दावा करता है कि वह सर्वोच्च सत्ता की चमक या प्रतिभा का प्रतीक है, जो व्यक्तियों को आध्यात्मिक संतुष्टि और उनके वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के लिए उनकी शरण लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।
साखी – परचा कौ अंग
कबीर तेज अनंत का, मानी ऊगी सूरज सेणि।
पति संगि जागी सूंदरी, कौतिग दीठा तेणि॥1॥
इस दोहे में, कबीर ने दिव्य प्रकाश और आध्यात्मिक मिलन के विचार को काव्यात्मक रूप से व्यक्त किया है। वह खुद की तुलना अनंत की चमक से करता है, यह सुझाव देता है कि उसका सार परमात्मा की प्रतिभा और असीमता को दर्शाता है। अपने पति की उपस्थिति में जागती एक खूबसूरत महिला की कल्पना आत्मा के जागरण या परमात्मा के साथ उसके वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति का प्रतीक है। इसी तरह, मोती का अपने खोल के भीतर दिखाई देना आंतरिक सुंदरता और सच्चाई के प्रकट होने का प्रतीक है। कुल मिलाकर, यह कविता आध्यात्मिक जागृति और स्वयं के भीतर दिव्य उपस्थिति की पहचान के विषय को बताती है
कोतिग दीठा देह बिन, मसि बिना उजास।
साहिब सेवा मांहि है, बेपरवांही दास॥2॥
इस दोहे में, कबीर आध्यात्मिक सत्य को व्यक्त करने के लिए रूपक भाषा का प्रयोग करते हैं। उनका सुझाव है कि सच्ची अनुभूति और रोशनी तब होती है जब कोई व्यक्ति भौतिक शरीर और भौतिक आसक्तियों से परे चला जाता है। शरीर के बिना मोती को देखने और मांस के बिना मौजूद प्रकाश की कल्पना भौतिक रूपों से परे सार को समझने के विचार को दर्शाती है। कबीर इस बात पर जोर देते हैं कि गुरु (परमात्मा या आध्यात्मिक मार्गदर्शक का प्रतिनिधित्व) की सेवा करना एक आंतरिक मामला है, जो दर्शाता है कि यह केवल बाहरी कार्यों के बजाय दिल और आत्मा का मामला है। बिना किसी दूसरे विचार के सेवक बनने की धारणा आध्यात्मिक यात्रा में संपूर्ण हृदय से समर्पण और समर्पण के महत्व को रेखांकित करती है।
पारब्रह्म के तेज का, कैसा है उनमान।
कहिबे कूं सोभा नहीं, देख्याही परवान॥3॥
इस दोहे में, कबीर सर्वोच्च सत्ता की प्रतिभा की अवर्णनीय प्रकृति को दर्शाते हैं। उनका सुझाव है कि ईश्वर की महिमा और महिमा का वर्णन करने के लिए शब्द अपर्याप्त हैं। इसके बजाय, किसी को इसकी भव्यता को वास्तव में समझने और सराहने के लिए इसका प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिए। कबीर का तात्पर्य है कि केवल ईश्वरीय महिमा के बारे में बात करना उसके साथ न्याय नहीं करता; वास्तव में योग्य या मान्य बनने के लिए व्यक्ति को इसे व्यक्तिगत रूप से देखना चाहिए। कविता इस विचार को रेखांकित करती है कि आध्यात्मिक अनुभूति मौखिक विवरण और बौद्धिक समझ से परे है, दिव्य ज्ञान की ओर यात्रा में प्रत्यक्ष अनुभव के महत्व पर जोर देती है।
अगम अगोचर गमि नहीं, तहां जगमगै जोति।
जहाँ कबीरा बंदिगी, ‘तहां’पाप पुन्य नहीं छोति॥4॥
इस दोहे में कबीर ईश्वरीय क्षेत्र की प्रकृति पर प्रकाश डालते हैं। उनका सुझाव है कि परमात्मा, जो समझ और धारणा से परे है, उसकी उज्ज्वल रोशनी से पहचाना जाता है। कबीर फिर इस बात पर जोर देते हैं कि जिस क्षेत्र में कबीरा की सच्ची पूजा (ईश्वरीय या सच्चे आध्यात्मिक मार्ग का प्रतिनिधित्व) मौजूद है, वहां पाप या पुण्य का कोई प्रभाव नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि सच्ची आध्यात्मिक भक्ति पाप और पुण्य जैसी सांसारिक अवधारणाओं के द्वंद्व से परे है, जो शुद्ध चेतना और मुक्ति की स्थिति की ओर ले जाती है। यह श्लोक इस विचार को रेखांकित करता है कि वास्तविक आध्यात्मिक अभ्यास व्यक्ति को नैतिक द्वंद्व की सीमाओं से परे दिव्य प्राप्ति की स्थिति की ओर ले जाता है।
हदे छाड़ि बेहदि गया, हुवा निरंतर बास।
कवल ज फूल्या फूल बिन, को निरषै निज दास॥5॥
इस दोहे में, कबीर ने एक ऐसे आत्मज्ञानी की पारलौकिक स्थिति का वर्णन किया है, जिसने सभी सीमाओं और सीमाओं को पार कर शाश्वत अस्तित्व की स्थिति प्राप्त कर ली है। बिना किसी चिंता या चिंता के खिलने वाले फूल का रूपक आध्यात्मिक अनुभूति के स्वाभाविक प्रकटीकरण को दर्शाता है। इसके बाद कबीर ने एक अलंकारिक प्रश्न उठाया और सुझाव दिया कि जिस प्रकार फूल को खिलने से कोई नहीं रोक सकता, उसी प्रकार आध्यात्मिक पथ के प्रति समर्पित सच्चे भक्त के मार्ग में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता। यह श्लोक दैवीय इच्छा के प्रति समर्पण करने और आध्यात्मिक विकास को सहजता से विकसित होने देने के विचार पर प्रकाश डालता है।
कबीर मन मधुकर भया, रह्या निरंतर बास।
कवल ज फूल्या जलह बिन, को देखै निज दास॥6॥
इस दोहे में, कबीर ने दिव्य आनंद में लीन होने की अपनी स्थिति का वर्णन करने के लिए फूलों की सुगंध से मदहोश मधुमक्खी के रूपक का उपयोग किया है। मधुमक्खी लगातार फूल के रस में डूबी रहती है, जो कबीर के परमात्मा के साथ अटूट संबंध का प्रतीक है। इसी तरह, जिस तरह एक फूल पानी जैसे बाहरी सहारे के बिना स्वाभाविक रूप से खिलता है, कबीर का तात्पर्य है कि उनका आध्यात्मिक अहसास बाहरी कारकों पर निर्भरता के बिना सहजता से खिलता है। इसके बाद उन्होंने एक अलंकारिक प्रश्न उठाया और सुझाव दिया कि जिस प्रकार विनम्र सेवक पर कोई ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार भक्ति और समर्पण की गहराई को केवल परमात्मा ही समझ सकता है। यह श्लोक परमात्मा में आंतरिक अवशोषण के विचार और आध्यात्मिक प्राप्ति के मार्ग में बाहरी मान्यता के महत्व पर जोर देता है।
अंतर कवल प्रकासिया, ब्रह्म बास तहां होइ।
मन भवरा तहां लुबधिया, जांणैगा जन कोइ॥7॥
इस दोहे में, कबीर उस आंतरिक रोशनी की बात करते हैं जो उस क्षेत्र में मौजूद है जहां ब्रह्मा, परम वास्तविकता, निवास करते हैं। उनका सुझाव है कि सच्चा ज्ञान और आध्यात्मिक बोध भीतर पाया जाता है, जहां दिव्य उपस्थिति प्रकट होती है। कबीर उन लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली आंतरिक शांति और संतुष्टि की तुलना करते हैं जिनका मन इस दिव्य क्षेत्र में लीन है और सामान्य मन की बेचैनी के साथ। उनका तात्पर्य यह है कि केवल कुछ ही व्यक्ति वास्तव में अंदर की ओर मुड़ने और आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के महत्व को समझते हैं। यह कविता आंतरिक रोशनी के महत्व और इसे समझने और प्राप्त करने वालों की दुर्लभता पर जोर देती है।
सायर नाहीं सीप बिन, स्वाति बूँद भी नाहिं।
कबीर मोती नीपजै, सुन्नि सिषर गढ़ माँहिं॥8॥
इस दोहे में, कबीर गहन आध्यात्मिक सच्चाइयों को व्यक्त करने के लिए रूपकों का उपयोग करते हैं। पहली पंक्ति ब्रह्मांड में विभिन्न तत्वों की परस्पर निर्भरता का सुझाव देती है; जिस प्रकार धोबी के बिना कपड़ा साफ नहीं किया जा सकता और तारों की उपस्थिति के बिना बारिश नहीं हो सकती, उसी प्रकार अस्तित्व में हर चीज एक-दूसरे से जुड़ी हुई है और एक-दूसरे पर निर्भर है।
दूसरी पंक्ति में, कबीर समुद्र में मोती बनने और फिर एक खाली सीप में पाए जाने की कल्पना का उपयोग करते हैं। यह रूपक आध्यात्मिक अनुभूति की यात्रा का प्रतीक है। सागर चेतना या दिव्य उपस्थिति के विशाल विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है, और मोती आत्मज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान के सार का प्रतीक है। कबीर सुझाव देते हैं कि सच्चा अहसास व्यक्ति के अस्तित्व की शून्यता के भीतर होता है, जैसे एक खाली खोल के भीतर एक कीमती मोती की खोज।
कुल मिलाकर, कविता अस्तित्व के अंतर्संबंध और इस विचार पर जोर देती है कि आध्यात्मिक अनुभूति व्यक्ति के अपने अस्तित्व की गहराई के भीतर से उत्पन्न होती है।
घट माँहे औघट लह्या, औघट माँहैं घाट।
कहि कबीर परचा भया, गुरु दिखाई बाट॥9॥
इस दोहे में, कबीर आध्यात्मिक सत्य को व्यक्त करने के लिए घड़े और घड़े के रूपक का उपयोग करते हैं। “बर्तन” व्यक्तिगत आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि “घड़ा” दिव्य या सभी अस्तित्व के स्रोत का प्रतीक है। कबीर सुझाव देते हैं कि व्यक्तिगत आत्मा परमात्मा से निकलती है, जैसे घड़े के भीतर से घड़ा निकाला जाता है। हालाँकि, परमात्मा व्यक्ति की आत्मा के भीतर उसी तरह रहता है, जैसे घड़ा घड़े के भीतर रहता है।
कबीर फिर दावा करते हैं कि व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा के बीच इस रिश्ते का रहस्य गुरु, आध्यात्मिक शिक्षक द्वारा प्रकट किया गया है। गुरु इस गहन सत्य को समझने का मार्ग दिखाते हैं और साधक को आध्यात्मिक प्राप्ति के मार्ग पर ले जाते हैं।
कुल मिलाकर, यह श्लोक व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा के बीच घनिष्ठ संबंध और आध्यात्मिक समझ और ज्ञानोदय को सुविधाजनक बनाने में गुरु की भूमिका पर जोर देता है।
सूर समांणो चंद में, दहूँ किया घर एक।
मनका च्यंता तब भया, कछू पूरबला लेख॥10॥
इस दोहे में कबीर आध्यात्मिक सत्य को व्यक्त करने के लिए रूपक भाषा का प्रयोग करते हैं। सूर्य दिव्य चेतना का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि चंद्रमा मन या व्यक्तिगत आत्म का प्रतीक है। कबीर सुझाव देते हैं कि दिव्य चेतना और व्यक्तिगत स्व दोनों एक ही ब्रह्मांडीय निवास के भीतर मौजूद हैं, जो व्यक्ति और परमात्मा के बीच अंतर्निहित एकता का संकेत देता है।
कबीर फिर उस क्षण का वर्णन करते हैं जब मन चिंतित या परेशान हो गया था। यह गड़बड़ी तब होती है जब व्यक्ति को दिव्य चेतना के साथ अपने संबंध का एहसास होता है, जिसके परिणामस्वरूप धारणा या समझ में गहरा बदलाव होता है। कबीर का तात्पर्य है कि यह अनुभूति असाधारण और परिवर्तनकारी है, जो आध्यात्मिक जागृति या आत्मज्ञान की ओर ले जाती है।
कुल मिलाकर, यह कविता व्यक्ति के भीतर रहने वाले परमात्मा की अवधारणा और इस अंतर्निहित एकता को साकार करने के परिवर्तनकारी प्रभाव को रेखांकित करती है।
हद छाड़ि बेहद गया, किया सुन्नि असनान।
मुनि जन महल न पावई, तहाँ किया विश्राम॥11॥
इस दोहे में, कबीर किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति का वर्णन करते हैं जिसने सभी सीमाओं को पार कर गहन शांति की स्थिति प्राप्त कर ली है। व्यक्ति ने सीमित दुनिया की सीमाओं को पार कर लिया है और आंतरिक शांति की गहरी भावना का अनुभव किया है। कबीर इस स्थिति की तुलना तपस्वी ऋषियों (मुनियों) द्वारा महल को खोजने में असमर्थता से करते हैं, जो परम सत्य या दिव्य अनुभूति का प्रतीक है। अपने प्रयासों और त्याग के बावजूद, वे अंतिम मंजिल को प्राप्त नहीं कर सके।
कबीर ने यह आलंकारिक प्रश्न उठाया है कि अगर इन तपस्वियों को महल भी नहीं मिला तो उन्हें आराम कहां मिलेगा, और सुझाव दिया कि सच्चा आराम या शांति केवल दैवीय सत्य की प्राप्ति में ही मिल सकती है। यह कविता आध्यात्मिक उत्कृष्टता और आंतरिक शांति और प्राप्ति की अंतिम खोज के विषय पर जोर देती है।
देखौ कर्म कबीर का, कछु पूरब जनम का लेख।
जाका महल न मुनि लहैं, सो दोसत किया अलेख॥12॥
इस दोहे में, कबीर अपने कार्यों और अपने पिछले जन्मों के परिणामों के बारे में बात करते हैं। उनका सुझाव है कि उनके वर्तमान कार्य पिछले जन्मों में संचित कर्मों से प्रभावित हैं। कबीर परम सत्य या ईश्वरीय अनुभूति को दर्शाने के लिए महल के रूपक का उपयोग करते हैं। उनका तात्पर्य यह है कि यहां तक कि तपस्वी ऋषि भी, जिन्होंने सांसारिक आसक्तियों और गतिविधियों को त्याग दिया है, इस परम सत्य को प्राप्त नहीं कर सके।
कबीर फिर इस परम सत्य को एक मित्र के रूप में वर्णित करते हैं, जो एक घनिष्ठ और अंतरंग रिश्ते का संकेत देता है। हालाँकि, उनका दावा है कि यह मित्र वर्णन (लेख) से परे है, जिसका अर्थ है कि यह शब्दों या समझ से परे है।
कुल मिलाकर, यह कविता पिछले कार्यों के परिणामों और अंतिम सत्य या दिव्य प्राप्ति की अक्षमता को समझने के महत्व पर जोर देती है। यह आध्यात्मिक खोज और आंतरिक अनुभूति की खोज के विषय पर जोर देता है।
पिंजर प्रेमे प्रकासिया, जाग्या जोग अनंत।
कुल मिलाकर, यह कविता दिव्य प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति और परमात्मा के साथ मिलन के माध्यम से आध्यात्मिक मुक्ति की प्राप्ति पर जोर देती है। यह भक्ति, आध्यात्मिक जागृति और आंतरिक पूर्णता की खोज के विषयों को रेखांकित करता है।
प्यंजर प्रेम प्रकासिया, अंतरि भया उजास।
मुख कसतूरी महमहीं, बांणीं फूटी बास॥14॥
इस दोहे में, कबीर व्यक्तिगत आत्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए पिंजरे के रूपक का उपयोग करते हैं, जो दिव्य प्रेम से प्रकाशित होता है। यह दिव्य प्रेम जागरूकता और आध्यात्मिक अनुभूति की आंतरिक रोशनी को सामने लाता है। कस्तूरी मृग द्वारा सुगंध के स्रोत को बाहर खोजने का संदर्भ बाहरी वस्तुओं और अनुभवों में खुशी और संतुष्टि की तलाश करने की मानवीय प्रवृत्ति का प्रतीक है, इस बात से अनजान कि खुशी का असली स्रोत भीतर है।
कबीर सुझाव देते हैं कि, कस्तूरी मृग की तरह, व्यक्ति अक्सर आनंद के आंतरिक स्रोत को नजरअंदाज कर देते हैं, और इसे बाहरी रूप से खोजते हैं। हालाँकि, जैसे ही कस्तूरी मृग को अंततः पता चलता है कि सुगंध उसके अपने शरीर के भीतर से निकलती है, व्यक्तियों को यह एहसास हो सकता है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि आध्यात्मिक अनुभूति के माध्यम से उनके भीतर पाई जाती है।
कुल मिलाकर, यह कविता अंदर की ओर मुड़ने और दिव्य प्रेम और आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से खुशी और संतुष्टि के आंतरिक स्रोत की खोज करने के महत्व पर जोर देती है। यह आंतरिक बोध और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज के विषय को रेखांकित करता है।
मन लागा उन मन्न सों, गगन पहुँचा जाइ।
देख्या चंदबिहूँणाँ, चाँदिणाँ, तहाँ अलख निरंजन राइ॥15॥
इस दोहे में, कबीर ने आध्यात्मिक धुन और अनुभूति के अनुभव का वर्णन किया है। उनका सुझाव है कि जब मन केंद्रित होता है और प्रिय के प्रति समर्पित होता है, तो यह सांसारिक सीमाओं को पार कर जाता है और आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, जिसका प्रतीक आकाश है। यह सामंजस्य निराकार और बेदाग क्षेत्र के अनुभव की ओर ले जाता है, जहां दिव्य उपस्थिति का एहसास होता है।
इसके बाद कबीर शांति और सुंदरता की भावना पैदा करने के लिए चांदनी रातों की कल्पना का उपयोग करते हैं। चांदनी रातें आध्यात्मिक स्पष्टता और रोशनी के क्षणों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जहां परमात्मा को उसके शुद्ध, निराकार रूप में देखा जाता है। इस क्षेत्र में, कबीर का सुझाव है, भौतिक संसार की सीमाओं से परे, वास्तविकता की निराकार, बेदाग प्रकृति का रहस्योद्घाटन है।
कुल मिलाकर, यह कविता सांसारिक सीमाओं को पार करने और अपने शुद्धतम रूप में दिव्य उपस्थिति का अनुभव करने में आध्यात्मिक भक्ति और सामंजस्य के महत्व पर जोर देती है। यह आध्यात्मिक अनुभूति और प्रिय के साथ मिलन की खोज के विषय को रेखांकित करता है
मन लागा उन मन सों, उन मन मनहि बिलग।
लूँण बिलगा पाणियाँ, पाँणीं लूँणा बिलग॥16॥
इस दोहे में, कबीर मिलन या विलय की अवधारणा को दर्शाने के लिए नमक और पानी के रूपक का उपयोग करते हैं। उनका सुझाव है कि जब मन पूरी तरह से समर्पित हो जाता है और प्रिय के प्रति समर्पित हो जाता है, तो वह उस प्रिय के साथ पूरी तरह से विलीन हो जाता है, जैसे नमक और पानी एक साथ मिल जाते हैं।
कबीर की सादृश्यता का तात्पर्य व्यक्तिगत स्वयं और प्रिय के बीच पूर्ण एकता और सीमाओं के विघटन की स्थिति से है। जिस प्रकार नमक घुलकर पानी में एक हो जाता है, उसी प्रकार व्यक्तिगत आत्मा भी घुलकर परमात्मा में एक हो जाती है। यह रूपक आध्यात्मिक मिलन के विषय और दिव्य उपस्थिति के साथ विलय के अंतिम लक्ष्य को रेखांकित करता है।
कुल मिलाकर, यह श्लोक आध्यात्मिक प्राप्ति के मार्ग में आध्यात्मिक भक्ति और मिलन के महत्व पर जोर देता है, जो प्रिय के साथ एकता और एकता की अवधारणा को दर्शाता है।
पाँणी ही तें हिम भया, हिम ह्नै गया बिलाइ।
जो कुछ था सोई भया, अब कछू कह्या न जाइ॥17॥
इस दोहे में, कबीर अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति को चित्रित करने के लिए पानी के बर्फ में बदलने और फिर पिघलने के रूपक का उपयोग करते हैं। पानी का बर्फ में जमना सांसारिक रूपों के जमने या प्रकट होने का प्रतीक है, जबकि बर्फ का वापस पानी में पिघलना उन रूपों के विघटन या नश्वरता का प्रतिनिधित्व करता है।
कबीर सुझाव देते हैं कि जो कुछ भी जमी हुई अवस्था में था, एक बार जब वह पिघल जाता है, तो कुछ भी नहीं बचता है। इसकी व्याख्या सांसारिक घटनाओं की क्षणिक प्रकृति और सभी भौतिक रूपों के अंतिम विघटन पर प्रतिबिंब के रूप में की जा सकती है। इस नश्वरता के सामने, कबीर का तात्पर्य है कि समझने या कहने के लिए कुछ भी ठोस या स्थायी नहीं है।
कुल मिलाकर, यह कविता नश्वरता के विषय और सांसारिक अस्तित्व की भ्रामक प्रकृति पर जोर देती है। यह जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति पर चिंतन और क्षणभंगुर के बीच शाश्वत की तलाश के महत्व को प्रोत्साहित करता है।
भली भई जु भै पड्या, गई दशा सब भूलि।
पाला गलि पाँणी भया, ढुलि मिलिया उस कूलि॥18॥
इस दोहे में, कबीर समर्पण या सांसारिक चिंताओं और आसक्तियों को त्यागने के अनुभव को दर्शाते हैं। वह गिरने के उस क्षण के लिए आभार व्यक्त करता है, जिसने उसे सभी बाहरी परिस्थितियों और विकर्षणों को भूलने की अनुमति दी। इस गिरावट की व्याख्या रूपक रूप से समर्पण या आध्यात्मिक जागृति की स्थिति के रूप में की जा सकती है, जहां व्यक्ति अहंकार और सांसारिक इच्छाओं के प्रति लगाव को छोड़ देता है।
कबीर फिर एक धारा के बहने और समुद्र में विलीन होने की कल्पना का उपयोग व्यक्तिगत आत्मा के परमात्मा के साथ मिलन के प्रतीक के रूप में करते हैं। जिस प्रकार धारा अपनी पहचान खो देती है और सागर की विशालता में विलीन हो जाती है, कबीर सुझाव देते हैं कि समर्पण की स्थिति में, व्यक्तिगत आत्मा आध्यात्मिक मुक्ति और पूर्णता प्राप्त करते हुए दिव्य चेतना में विलीन हो जाती है।
चौहटै च्यंतामणि चढ़ी, हाडी मारत हाथि।
मीरा मुझसूँ मिहर करि, इब मिलौं न काहू साथि॥19॥
इस कविता में, मीराबाई अपनी आध्यात्मिक यात्रा और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को व्यक्त करने के लिए रूपक भाषा का उपयोग करती हैं। “छत” आध्यात्मिक पथ का प्रतीक है, और “इच्छा-पूर्ति करने वाला रत्न” दिव्य प्राप्ति या कृष्ण के साथ मिलन की उसकी खोज का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे वह अपना प्रिय मानती थी। हालाँकि, आध्यात्मिक संतुष्टि पाने के बजाय, उसे चमगादड़ द्वारा हमला करने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
इस झटके के बावजूद, मीराबाई को अपने प्रिय कृष्ण के करुणामय शब्दों में सांत्वना मिलती है। वह इस अनुभव की व्याख्या एक संकेत के रूप में करती है कि उसे बाहरी परिस्थितियों या साहचर्य पर निर्भरता के बिना, अपने आध्यात्मिक पथ पर अकेले चलना चाहिए।
पंषि उडाणी गगन कूँ, प्यंड रह्या परदेस।
पाँणी पीया चंच बिन, भूलि गया यहु देस॥20॥
इस दोहे में, कबीर गहन आध्यात्मिक सत्य को व्यक्त करने के लिए रूपक भाषा का उपयोग करते हैं। “पक्षी” व्यक्तिगत आत्मा या मनुष्य का प्रतीक है, जबकि “आकाश” अस्तित्व या आध्यात्मिक क्षेत्र के विशाल विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। आकाश में उड़ने के बावजूद, पक्षी का “घोंसला” या सच्चा घर दूर देश में है, जो बताता है कि व्यक्ति का असली सार भौतिक दुनिया से परे, परमात्मा के दायरे में है।
कबीर ने चंबल नदी का संदर्भ देकर इस बात को और स्पष्ट किया है, जो अपने गंदे और अशांत पानी के लिए जानी जाती है। चंबल नदी का पानी पीने से व्यक्ति अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप और मूल को भूलकर सांसारिक इच्छाओं और आसक्तियों में उलझ जाता है।
पंषि उड़ानी गगन कूँ, उड़ी चढ़ी असमान।
जिहिं सर मण्डल भेदिया, सो सर लागा कान॥21॥
इस दोहे में कबीर आध्यात्मिक सत्य को व्यक्त करने के लिए रूपक भाषा का प्रयोग करते हैं। “पक्षी” व्यक्तिगत आत्मा या मनुष्य का प्रतीक है, जबकि “आकाश” अस्तित्व या आध्यात्मिक क्षेत्र के असीम दायरे का प्रतिनिधित्व करता है। आकाश में पक्षी की उड़ान आध्यात्मिक मुक्ति या अतिक्रमण की खोज का सुझाव देती है।
इसके बाद कबीर सिर के काटे जाने और फिर से जोड़े जाने की अवधारणा का परिचय देते हैं। इस रूपक की व्याख्या जन्म और मृत्यु के चक्र या जीवन के अनुभवों के प्रतीक के रूप में की जा सकती है। कबीर सुझाव देते हैं कि व्यक्ति के सामने चाहे कितनी भी चुनौतियाँ या बाधाएँ आएँ, नवीनीकरण या पुनर्जनन की संभावना हमेशा बनी रहती है।
सुरति समाँणो निरति मैं, निरति रही निरधार।
सुरति निरति परचा भया, तब खूले स्यंभ दुवार॥22॥
इस दोहे में, कबीर ने गहन ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास में तल्लीनता के अपने अनुभव का वर्णन किया है। “सुरति” शब्द ध्यान या चिंतन को संदर्भित करता है, जबकि “निरति” अवशोषण या स्थिर होने का प्रतीक है। कबीर इंगित करते हैं कि वे बिना किसी बाहरी समर्थन या व्याकुलता के, अपने ध्यान अभ्यास में अटल रहे।
इसके बाद कबीर ध्यान और तल्लीनता के विलय की बात करते हैं, और परमात्मा के साथ पूर्ण मिलन या संरेखण की स्थिति का सुझाव देते हैं। यह विलय सर्वोच्च के द्वार खोलने की ओर ले जाता है, जो आध्यात्मिक अनुभूति या ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है।
सुरति समाँणो निरति मैं, अजपा माँहै जाप।
लेख समाँणाँ अलेख मैं, यूँ आपा माँहै आप॥23॥
इस दोहे में, कबीर ध्यान में अपनी गहरी व्यस्तता और अनकहे मंत्र (अजपा जप) के निरंतर दोहराव को व्यक्त करते हैं, जो निरंतर ध्यान और आंतरिक अवशोषण की स्थिति का संकेत देता है। “अजपा” शब्द मंत्र की पुनरावृत्ति को संदर्भित करता है जो सचेत प्रयास के बिना, अनायास और लगातार भीतर होता है।
कबीर तब आध्यात्मिक अनुभूति की गहन स्थिति को दर्शाने के लिए तल्लीनता के ग्रंथों में लिखे जाने के रूपक का उपयोग करते हैं। उनका सुझाव है कि यद्यपि उनकी तल्लीनता की स्थिति को आध्यात्मिक ग्रंथों में पहचाना और प्रलेखित किया गया है, लेकिन उनका वास्तविक सार वर्णन या वर्गीकरण से परे है। जिस प्रकार आत्मा स्वतंत्र रूप से और स्व-अस्तित्व में मौजूद है, कबीर का तात्पर्य है कि उनका आध्यात्मिक अहसास शब्दों या लिखित विवरणों से परे है।
आया था संसार में, देषण कौं बहु रूप।
कहै कबीरा संत ही, पड़ि गया नजरि अनूप॥24॥
इस दोहे में कबीर संसार में अस्तित्व की विविध अभिव्यक्तियों पर प्रकाश डालते हैं। वह अस्तित्व के दायरे में जीवन के असंख्य रूपों और दिखावे को स्वीकार करता है। हालाँकि, कबीर सुझाव देते हैं कि इस विविधता के बीच, केवल संत या आध्यात्मिक रूप से जागृत व्यक्ति ही हैं जो वास्तव में अस्तित्व की असाधारण प्रकृति को समझते हैं।
कबीर का तात्पर्य है कि संतों के पास एक विशेष अंतर्दृष्टि या दृष्टि होती है जो उन्हें दुनिया की सतही दिखावे से परे देखने और सभी सृष्टि में मौजूद अंतर्निहित एकता और दिव्य सार को पहचानने की अनुमति देती है। उनकी धारणा सामान्य से परे है और अस्तित्व की असाधारण सुंदरता और अंतर्संबंध को महसूस करती है।
अंक भरे भरि भेटिया, मन मैं नाँहीं धीर।
कहै कबीर ते क्यूँ मिलैं, जब लग दोइ सरीर॥25॥
इस दोहे में, कबीर औपचारिकताओं और दिखावे की विशेषता वाले सामाजिक संबंधों की सतहीता को दर्शाते हैं। उनका मानना है कि बैठकों और सभाओं के बाहरी दिखावे के बावजूद, मन में अक्सर वास्तविक जुड़ाव या स्थिरता की कमी होती है।
कबीर ऐसी बैठकों के उद्देश्य पर सवाल उठाते हैं जब इसमें शामिल व्यक्ति मन और आत्मा के स्तर पर अलग-थलग रहते हैं। उनका सुझाव है कि सच्चा संवाद और जुड़ाव तभी हो सकता है जब भौतिक शरीर की सीमाओं को पार करते हुए चेतना की एकता हो।
सचु पाया सुख ऊपनाँ, अरु दिल दरिया पूरि।
सकल पाप सहजै गये, जब साँई मिल्या हजूरि॥26॥
इस दोहे में, कबीर उस गहन आंतरिक परिवर्तन और आध्यात्मिक अनुभूति को दर्शाते हैं जो उन्होंने ईश्वर से मिलने पर अनुभव किया था। वह प्रतीकात्मक रूप से अपने भीतर सच्ची खुशी खोजने का वर्णन करता है, यह सुझाव देता है कि आध्यात्मिक संतुष्टि और संतुष्टि बाहरी स्रोतों के बजाय भीतर से उत्पन्न होती है।
कबीर अपने आध्यात्मिक अनुभव की विशालता और गहराई को व्यक्त करने के लिए हृदय के सागर बन जाने के रूपक का उपयोग करते हैं। उनका तात्पर्य यह है कि ईश्वर के साथ मिलन ने उनके हृदय को असीम प्रेम और करुणासे भर दिया, जिससे इसका विस्तार पूरे अस्तित्व में हो गया।
इसके अलावा, कबीर का दावा है कि ईश्वर के साथ मिलन के परिणामस्वरूप सभी पाप सहजता से नष्ट हो गए। इससे पता चलता है कि दिव्य उपस्थिति का एहसास और आध्यात्मिक मिलन का अनुभव व्यक्ति को पिछले कार्यों और नकारात्मक प्रवृत्तियों के बोझ से शुद्ध करने और मुक्त करने की शक्ति रखता है।
धरती गगन पवन नहीं होता, नहीं तोया, नहीं तारा।
तब हरि हरि के जन होते, कहै कबीर बिचारा॥27॥
इस दोहे में, कबीर अस्तित्व के मूल तत्वों पर विचार करते हैं: पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और तारे। उनका सुझाव है कि ब्रह्मांड के इन आवश्यक घटकों के बिना, मानव अस्तित्व के लिए कोई भौतिक क्षेत्र नहीं होगा।
हालाँकि, कबीर भौतिक क्षेत्र से परे जाकर एक गहरा सवाल उठाते हैं: इन भौतिक तत्वों की अनुपस्थिति में, भगवान के भक्त या अनुयायी कौन होंगे? वह भक्ति और आध्यात्मिकता की प्रकृति पर चिंतन को आमंत्रित करते हैं, जिसका अर्थ है कि इन तत्वों की उपस्थिति आध्यात्मिक अभ्यास और परमात्मा के प्रति समर्पण का अवसर प्रदान करती है।
जा दिन कृतमनां हुता, होता हट न पट।
हुता कबीरा राम जन, जिनि देखै औघट घट॥28॥
इस दोहे में, कबीर किसी के कार्यों के परिणामों पर विचार करते हैं, यह सुझाव देते हुए कि किसी के कार्यों के परिणामों या नतीजों से बचा नहीं जा सकता है। वह छुपाने या टालने की संभावना के बिना, अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने की अनिवार्यता पर जोर देता है।
इसके बाद कबीर सामान्य के भीतर असाधारण को समझने की अवधारणा का परिचय देते हैं। उनका सुझाव है कि राम या भगवान के सच्चे भक्त वे हैं जो जीवन के सांसारिक पहलुओं के भीतर दिव्य उपस्थिति को पहचानने की क्षमता रखते हैं। इसका तात्पर्य एक बढ़ी हुई जागरूकता और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से है जो व्यक्तियों को वास्तविकता की सतह से परे देखने और सभी चीजों में निहित गहरे आध्यात्मिक आयाम को समझने में सक्षम बनाता है।
थिति पाई मन थिर भया, सतगुर करी सहाइ।
अनिन कथा तनि आचरी, हिरदै त्रिभुवन राइ॥29॥
इस दोहे में, कबीर सच्चे गुरु, या आध्यात्मिक शिक्षक के मार्गदर्शन से मन के परिवर्तन और गहन सत्य के रहस्योद्घाटन पर विचार करते हैं। उनका सुझाव है कि गुरु की सहायता से, मन को स्थिरता और स्थिरता मिलती है, जिससे गहरी अंतर्दृष्टि और समझ मिलती है।
इसके बाद कबीर अनकही कहानी के उद्भव का वर्णन करते हैं, जिसका अर्थ है मौखिक अभिव्यक्ति से परे आध्यात्मिक सत्य का रहस्योद्घाटन। यह सत्य हृदय के भीतर रहता है, जो व्यक्ति के सबसे अंतरतम केंद्र का प्रतीक है जहां दिव्य ज्ञान और अनुभूति प्रकट होती है। इस सत्य के प्रकाश का गहरा प्रभाव पड़ता है, इसका प्रभाव तीनों लोकों तक फैल जाता है, जो इसके सार्वभौमिक महत्व को दर्शाता है।
हरि संगति सीतल भया, मिटा मोह की ताप।
निस बासुरि सुख निध्य लह्या, जब अंतरि प्रकट्या आप॥30॥
इस दोहे में, कबीर ईश्वरीय संगति की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाते हैं। वह शीतलता पाने का वर्णन करता है, जो ईश्वरीय संगति में आंतरिक शांति और शांति का प्रतीक है। यह संगति व्यक्ति को सांसारिक इच्छाओं और विकर्षणों से मुक्त करके, लगाव की जलन को कम करने में मदद करती है।
इसके बाद कबीर रात की ठंडी छाया में शांति पाने के रूपक का उपयोग करते हैं, जो गहरी शांति और संतुष्टि की स्थिति का सुझाव देते हैं जो तब उत्पन्न होती है जब भीतर दिव्य उपस्थिति का एहसास होता है। यह आंतरिक अहसास शांति के खजाने की खोज की ओर ले जाता है, जो उस गहन आध्यात्मिक संतुष्टि को दर्शाता है जो सीधे ईश्वर का अनुभव करने से आती है।
तन भीतरि मन मानियाँ, बाहरि कहा न जाइ।
ज्वाला तै फिरि जल भया, बुझी बलंती लाइ॥31॥
इस दोहे में, कबीर शरीर के भीतर मन के आंतरिक समर्पण को दर्शाते हैं, आंतरिक सद्भाव और एकीकरण की स्थिति का सुझाव देते हैं। उनका तात्पर्य यह है कि जब मन पूरी तरह से समर्पित हो जाता है और शरीर के भीतर लीन हो जाता है, तो यह बाहरी अभिव्यक्ति या विवरण से परे हो जाता है।
इसके बाद कबीर उस आग के रूपक का उपयोग करते हैं जो एक बार भयंकर रूप से जलती थी लेकिन अब बुझ गई है और अवशोषित हो गई है। यह रूपक आंतरिक उथल-पुथल और उत्तेजना को शांति और शांति की स्थिति में बदलने का प्रतिनिधित्व करता है। इच्छाओं, आसक्तियों और अहंकार की आग को आंतरिक समर्पण और अवशोषण के माध्यम से बुझा दिया गया है, जिससे आंतरिक शांति और शांति की अनुभूति हुई है।
तत पाया तन बीसर्या, जब मुनि धरिया ध्यान।
तपनि गई सीतल भया, जब सुनि किया असनान॥32॥
इस दोहे में, कबीर ध्यान और वैराग्य की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाते हैं। उनका सुझाव है कि अस्तित्व के सार का सच्चा अहसास तब प्राप्त होता है जब अभ्यासकर्ता भौतिक शरीर को भूल जाता है और ध्यान में लीन हो जाता है। जब भिक्षु ध्यान पर गहराई से ध्यान केंद्रित करता है, तो शरीर और उसकी चिंताएँ पृष्ठभूमि में फीकी पड़ जाती हैं, जिससे आध्यात्मिक अनुभूति का सार उभर कर सामने आता है।
फिर कबीर वैराग्य के प्रभाव को दर्शाने के लिए जलन और शीतलता के रूपक का उपयोग करते हैं। जलना सांसारिक इच्छाओं और चिंताओं के प्रति लगाव के कारण होने वाली उत्तेजना और पीड़ा को दर्शाता है। हालाँकि, वैराग्य को समझने और अभ्यास करने पर, यह जलन समाप्त हो जाती है, और शीतलता और शांति की भावना इसकी जगह ले लेती है। सांसारिक मोह-माया और इच्छाओं से वैराग्य से आंतरिक शांति मिलती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है।
जिनि पाया तिनि सू गह्या गया, रसनाँ लागी स्वादि।
रतन निराला पाईया, जगत ढंढाल्या बादि॥33॥
इस दोहे में कबीर आध्यात्मिक अनुभूति के गहन अनुभव को दर्शाते हैं। उनका सुझाव है कि जो लोग इस अनुभूति को प्राप्त कर लेते हैं वे इसे चुपचाप अपने भीतर ही रखते हैं, इसकी मिठास और गहराई को बाहरी रूप से व्यक्त करने के बजाय आंतरिक रूप से अनुभव करते हैं। इस आंतरिक अनुभव की तुलना किसी स्वादिष्ट चीज़ को चखने से की जाती है, जो गहरी संतुष्टि और तृप्ति को दर्शाता है।
इसके बाद कबीर आध्यात्मिक अनुभूति की दुर्लभता और बहुमूल्यता को दर्शाने के लिए एक अद्वितीय रत्न की खोज के रूपक का उपयोग करते हैं। यह अहसास संसार की क्षणभंगुरता और अनिश्चित प्रकृति से परे है, जो संसार के क्षणभंगुर तरीकों का प्रतीक है। यह एक कालातीत और स्थायी सत्य का प्रतिनिधित्व करता है जो व्यक्ति को जीवन की सांसारिक चिंताओं से ऊपर उठाता है।
कबीर दिल स्याबति भया, पाया फल सम्रथ्थ।
सायर माँहि ढंढोलताँ, हीरै पड़ि गया हथ्थ॥34॥
इस दोहे में कबीर आध्यात्मिक अनुभूति की प्राप्ति पर विचार करते हैं। उनका सुझाव है कि जब हृदय शुद्ध और अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है, तो आध्यात्मिक प्राप्ति सहज हो जाती है, जो किसी के प्रयासों का फल आसानी से प्राप्त करने के समान है।
इसके बाद कबीर संसार में जीवन की यात्रा के प्रतीक के रूप में बाज़ार में भटकने के रूपक का उपयोग करते हैं। सांसारिक अस्तित्व की विकर्षणों और चुनौतियों के बावजूद, हीरे द्वारा दर्शाया गया आध्यात्मिक खजाना अनायास ही हाथ में आ जाता है। इससे पता चलता है कि सच्ची आध्यात्मिक अनुभूति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती है, बल्कि जब हृदय शुद्ध और ग्रहणशील होता है तो स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है।
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाँहि।
सब अँधियारा मिटि गया, जब दीपक देख्या माँहि॥35॥
इस दोहे में, कबीर स्वयं के भीतर दिव्य उपस्थिति को महसूस करने के परिवर्तनकारी अनुभव को दर्शाते हैं। वह अस्तित्व की दो अवस्थाओं में विरोधाभास करता है: एक जहां वह ईश्वर के बारे में जागरूकता के बिना अस्तित्व में था, और दूसरा जहां ईश्वर उसके भीतर मौजूद है, और उसकी व्यक्तिगत पहचान मिट जाती है।
कबीर अंधेरे से प्रकाश की ओर गहन बदलाव का वर्णन करते हैं जो भीतर दिव्य उपस्थिति को पहचानने पर होता है। अंधकार अज्ञानता और आध्यात्मिक अंधेपन का प्रतीक है, जबकि प्रकाश दिव्य रोशनी और प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इस आंतरिक प्रकाश को देखने पर, सारा अंधकार और अज्ञान दूर हो जाता है, और दिव्य अस्तित्व का सत्य स्पष्ट हो जाता है।
जा कारणि मैं ढूंढता, सनमुख मिलिया आइ।
धन मैली पिव ऊजला, लागि न सकौं पाइ॥36॥
इस दोहे में कबीर अर्थ और पूर्ति की खोज पर विचार करते हैं। वह भौतिक संपदा की अशुद्धता की तुलना परमात्मा के साक्षात्कार की पवित्रता से करता है। कबीर ने अस्तित्व के कारण या उद्देश्य की खोज करते समय सीधे प्रिय या परमात्मा को खोजने का वर्णन किया है। इस मुठभेड़ को दैवीय उपस्थिति के साथ प्रत्यक्ष और अंतरंग मुलाकात के रूप में दर्शाया गया है।
इसके बाद कबीर भौतिक संपदा की, जो स्वाभाविक रूप से अशुद्ध है, परमात्मा की तुलना करते हैं, जो शुद्ध और बेदाग है। उनका सुझाव है कि चाहे कोई भी भौतिक धन प्राप्त करने की कितनी भी कोशिश कर ले, वह कभी भी सच्ची संतुष्टि या संतुष्टि नहीं लाएगा। इसके बजाय, सच्ची संतुष्टि परमात्मा के साक्षात्कार में मिलती है।
जा कारणि मैं जाइ था, सोई पाई ठौर।
सोई फिर आपण भया, जासूँ कहता और॥37॥
इस दोहे में, कबीर स्थिरता या अपनेपन की भावना की तलाश के विचार को दर्शाते हैं। उनका सुझाव है कि जिस स्थान की वह तलाश कर रहे थे, संभवतः बाहरी दुनिया में, वहीं अंततः उन्हें वह स्थिरता मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। इस स्थिरता की व्याख्या आंतरिक शांति, संतुष्टि या आध्यात्मिक अनुभूति की भावना के रूप में की जा सकती है।
कबीर फिर इस बात पर जोर देते हैं कि वह स्थान स्वयं उनका हो गया। इससे उस स्थान पर स्वामित्व या संबंध की गहरी भावना का पता चलता है जहां उसे स्थिरता मिली, यह दर्शाता है कि उसे वहां अपनेपन या संतुष्टि की भावना मिली।
कबीर देख्या एक अंग, महिमा कही न जाइ।
तेज पुंज पारस धणों, नैनूँ रहा समाइ॥38॥
इस दोहे में कबीर आध्यात्मिक अनुभूति के गहन अनुभव को दर्शाते हैं। वह एक अंग को देखने का वर्णन करता है, जो एक दिव्य या पारलौकिक इकाई का प्रतीक है। इस अंग की महिमा इतनी अपार है कि इसका पर्याप्त वर्णन या शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता।
कबीर फिर इस दिव्य इकाई की प्रकृति का वर्णन करने के लिए रूपकों का उपयोग करते हैं। वह इसकी तुलना प्रतिभा के सार से करते हुए एक गहन और उज्ज्वल उपस्थिति का सुझाव देते हैं। इसके अतिरिक्त, वह इसकी तुलना एक कसौटी से करता है, जिसमें चीजों की वास्तविक प्रकृति को बदलने या प्रकट करने की शक्ति होती है। अंत में, कबीर वर्णन करते हैं कि कैसे यह दिव्य उपस्थिति उनकी आँखों में विलीन हो जाती है, जिससे मिलन या अहसास का गहरा और अंतरंग आध्यात्मिक अनुभव होता है।
मानसरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराहिं।
मुकताहल मुकता चुगैं, अब उड़ि अनत न जाहिं॥39॥
इस दोहे में, कबीर आध्यात्मिक सत्य को व्यक्त करने के लिए रूपकों का उपयोग करते हैं। मानसरोवर झील हिंदू पौराणिक कथाओं में जल का एक पवित्र भंडार है, जो पवित्रता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। हंस, जिसे अक्सर पवित्रता और आध्यात्मिक अनुग्रह के प्रतीक के रूप में चित्रित किया जाता है, इस झील में खेलने के लिए चिल्लाता है, जो साधक की आध्यात्मिक पूर्ति और परमात्मा के साथ मिलन की लालसा का प्रतीक है।
कबीर फिर एक मुक्त पक्षी की बात करते हैं जो मोती चुगता है। यह पक्षी उस प्रबुद्ध आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है जिसने आध्यात्मिक मुक्ति या मोक्ष प्राप्त कर लिया है। भौतिक धन या मोतियों के प्रतीक सांसारिक इच्छाओं से मोहित होने के बजाय, मुक्त आत्मा अपने आध्यात्मिक सार में स्थिर रहती है और इससे दूर नहीं भटकती है।
गगन गरिजि अमृत चवै, कदली कंवल प्रकास।
तहाँ कबीरा बंदिगी, कै कोई निज दास॥40॥
इस दोहे में, कबीर आध्यात्मिक सच्चाइयों को व्यक्त करने के लिए ज्वलंत कल्पना का उपयोग करते हैं। वह आकाश की गड़गड़ाहट का वर्णन करता है, जिसे ब्रह्मांड में गूंजती दिव्य उपस्थिति के रूपक के रूप में समझा जा सकता है। गड़गड़ाहट के साथ जुड़े अमृत के स्वाद का तात्पर्य आध्यात्मिक अनुभूति के आनंद और मिठास से है।
इसके बाद कबीर ने केले के पौधों और कमलों का उल्लेख किया, जो पवित्रता और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक हैं। उनकी चमक आत्मज्ञान की चमक और आध्यात्मिक जागृति की सुंदरता का प्रतिनिधित्व करती है।
अंत में, कबीर स्वयं को इस दिव्य उपस्थिति में पूजा करने की बात करते हैं। अपनी श्रद्धा और भक्ति के बावजूद, वह सवाल करते हैं कि क्या वास्तव में ईश्वर की सेवा करने वाला कोई है, जो वास्तविक भक्ति और निस्वार्थ सेवा की दुर्लभता को दर्शाता है।
नींव बिहुणां देहुरा, देह बिहूँणाँ देव।
कबीर तहाँ बिलंबिया करे अलप की सेव॥41॥
इस दोहे में, कबीर भौतिक शरीर की क्षणिक प्रकृति और भौतिक अस्तित्व की नश्वरता को व्यक्त करने के लिए रूपक भाषा का प्रयोग करते हैं। इमारत की नींव की तुलना रेत से करने से शरीर की नाजुकता और अस्थायी प्रकृति का पता चलता है। जिस प्रकार रेत पर बनी संरचना अस्थिर और नश्वर होती है, उसी प्रकार अस्तित्व की भव्य योजना में शरीर भी अस्थिर है।
फिर कबीर इस अस्थायी निवास में थोड़ी सेवा करने का सुझाव देते हैं। इसकी व्याख्या जीवन और भौतिक शरीर की क्षणिक प्रकृति के बावजूद, किसी के जीवनकाल के दौरान दया, करुणा और निस्वार्थता के कार्यों में संलग्न होने के रूप में की जा सकती है। कबीर वर्तमान क्षण का अधिकतम लाभ उठाने और पृथ्वी पर अपने समय का उपयोग दूसरों की सेवा करने और भौतिक क्षेत्र से परे गुणों को विकसित करने की वकालत करते हैं।
देवल माँहै देहुरी, तिल जेहैं बिसतार।
माँहैं पाती माँहिं जल, माँहे पुजणहार॥42॥
इस दोहे में, कबीर मानव शरीर और उसके आध्यात्मिक महत्व का वर्णन करने के लिए रूपक भाषा का उपयोग करते हैं। उन्होंने आध्यात्मिक यात्रा में इसकी पवित्रता और महत्व पर जोर देते हुए शरीर की तुलना एक मंदिर से की है। जिस प्रकार एक मंदिर पूजा और श्रद्धा का स्थान है, उसी प्रकार मानव शरीर भी आध्यात्मिक अनुभव और अनुभूति का एक पात्र है।
कबीर ने चारों ओर बिखरे तिलों का उल्लेख किया है, जो शरीर को घेरने वाले सांसारिक मोह-माया और विकर्षणों की अनित्य और क्षणिक प्रकृति का प्रतीक हो सकते हैं। इन विकर्षणों के बावजूद, कबीर हमें शरीर के भीतर की पवित्रता की याद दिलाते हैं।
वह आगे इस बात पर जोर देते हैं कि शरीर के भीतर पत्तियां और पानी हैं, जो आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक पवित्रता और जीविका के तत्वों का प्रतीक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कबीर का दावा है कि जिसकी पूजा की जानी चाहिए, या परमात्मा, वह शरीर के भीतर ही रहता है। यह इस विचार को उजागर करता है कि पूजा और श्रद्धा का असली उद्देश्य बाहरी नहीं है बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर रहता है।
कबीर कवल प्रकासिया, ऊग्या निर्मल सूर।
निस अँधियारी मिटि गई, बाजै अनहद तूर॥43॥
इस दोहे में, कबीर परमात्मा की उज्ज्वल प्रकृति और उसकी परिवर्तनकारी शक्ति का जश्न मनाते हैं। उनका दावा है कि केवल परमात्मा के पास ही सच्ची चमक है, और इसकी तुलना उन्होंने शुद्ध और उज्ज्वल सूर्य से की है। यह कल्पना दिव्य उपस्थिति की प्रतिभा और स्पष्टता का सुझाव देती है, जो अज्ञान और झूठ के अंधेरे को उजागर करती है।
कबीर फिर घोषणा करते हैं कि परमात्मा की उपस्थिति में सारा अंधकार गायब हो गया है। यह आध्यात्मिक अज्ञान को दूर करने और सत्य और ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। अंधेरे के गायब होने के साथ, कबीर ने अप्रकाशित राग की गूंज का वर्णन किया है, जो अस्तित्व में व्याप्त सद्भाव और दिव्य प्रतिध्वनि का प्रतीक है।
अनहद बाजै नीझर झरै, उपजै ब्रह्म गियान।
अविगति अंतरि प्रगटै, लागै प्रेम धियान॥44॥
इस दोहे में, कबीर आध्यात्मिक ज्ञान और दिव्य प्राप्ति के विषय का पता लगाना जारी रखते हैं। वह हिंदू और सिख आध्यात्मिकता में शाश्वत और अनुपचारित ध्वनि कंपन, अनाहद नाद का जिक्र करते हुए, बिना रुके ध्वनि का वर्णन करके शुरुआत करते हैं। इस ध्वनि को सृष्टि में अंतर्निहित ब्रह्मांडीय कंपन माना जाता है और अक्सर इसे दिव्य प्रतिध्वनि और ज्ञानोदय से जोड़ा जाता है।
इसके बाद कबीर दिव्य ज्ञान के प्रवाह की बात करते हैं और इसकी तुलना उस धारा से करते हैं जो निरंतर बहती रहती है और साधक की आत्मा को पोषण देती है। यह दिव्य ज्ञान परिवर्तनकारी है और आध्यात्मिक जागृति और ज्ञानोदय की ओर ले जाता है।
दोहे के अगले भाग में, कबीर हृदय के गुप्त कक्ष में आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति का उल्लेख करते हैं, जो किसी के अस्तित्व की अंतरतम गहराई का सुझाव देता है जहां आध्यात्मिक अनुभूति होती है। यहां, आत्मज्ञान स्पष्ट हो जाता है, जो साधक की चेतना को दिव्य समझ और अंतर्दृष्टि से प्रकाशित करता है।
आकासै मुखि औंधा कुवाँ, पाताले पनिहारि।
ताका पाँणीं को हंसा पीवै, बिरला आदि बिचारि॥45॥
इस दोहे में, कबीर गहन आध्यात्मिक सच्चाइयों को व्यक्त करने के लिए रूपक भाषा का प्रयोग करते हैं। अंधा कौआ अज्ञानता और भौतिकता के प्रति लगाव का प्रतीक है, क्योंकि यह आकाश से पीता है, जो दुनिया के बाहरी, क्षणिक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसके विपरीत, हंस, जो अक्सर शुद्धता और आध्यात्मिक अनुग्रह से जुड़ा होता है, अंडरवर्ल्ड के अमृत जल से पीता है, जो आध्यात्मिक सार और आंतरिक अहसास की खोज का प्रतीक है।
कबीर ने एक अलंकारिक प्रश्न उठाया: हंस किसका पानी पीता है? यहां, वह सच्चे आध्यात्मिक पोषण के स्रोत पर चिंतन को आमंत्रित करता है। जहां अंधा कौआ सांसारिक कार्यों में उलझा रहता है, वहीं हंस दिव्य तत्व की तलाश में रहता है। हालाँकि, कबीर सुझाव देते हैं कि लोग शायद ही कभी अपने आध्यात्मिक भरण-पोषण के मूल या स्रोत पर विचार करते हैं। प्रतिबिंब की यह कमी व्यक्तियों को अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति और परमात्मा के साथ उनके संबंध को समझने से रोकती है।
सिव सकती दिसि कौंण जु जोवै, पछिम दिस उठै धूरि।
जल मैं स्यंघ जु घर करै, मछली चढ़ै खजूरि॥46॥
इस दोहे में, कबीर गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि व्यक्त करने के लिए रूपक भाषा का उपयोग करते हैं। शिव दिव्य मर्दाना सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शक्ति दिव्य स्त्री सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है। कबीर पूछते हैं कि इन दो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के मिलन को कौन समझ सकता है। यह मिलन ब्रह्मांड के भीतर विरोधाभासों के सामंजस्य और संतुलन का प्रतीक है, जिसमें मर्दाना और स्त्रीत्व, सक्रिय और निष्क्रिय, या भौतिक और आध्यात्मिक पहलू शामिल हैं।
इसके बाद कबीर पश्चिम दिशा में धूल के उड़ने का उल्लेख करते हैं, जिसे रूपक के रूप में भौतिक संसार के विकर्षणों और भ्रमों के रूप में समझा जा सकता है जो आध्यात्मिक धारणा में बाधा डालते हैं। आध्यात्मिक प्रतीकवाद में पश्चिमी दिशा को अक्सर अंधकार या अज्ञान से जोड़ा जाता है।
अमृत बरसै हीरा निपजै, घंटा पड़ै टकसाल।
कबीर जुलाहा भया पारषू, अगभै उतर्या पार॥47॥
इस दोहे में, कबीर आध्यात्मिक सत्य को व्यक्त करने के लिए रूपकों का उपयोग करते हैं। अमृत की वर्षा और हीरे बिखरने की कल्पना प्रचुरता और आध्यात्मिक संपदा का संकेत देती है। हथौड़े से निहाई का बजना आध्यात्मिक अभ्यास की परिवर्तनकारी प्रक्रिया का प्रतीक है, जहां कच्चे माल को प्रयास और अनुशासन के माध्यम से आकार और परिष्कृत किया जाता है।
इसके बाद कबीर ने लाक्षणिक रूप से खुद को एक जुलाहा बताया। बुनाई का कार्य आध्यात्मिक परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रतीक है, जहां अनुभव और समझ के अलग-अलग धागों को एक साथ जोड़कर एक एकीकृत संपूर्णता का निर्माण किया जाता है। जिस प्रकार एक बुनकर कच्चे कपड़े को बढ़िया कपड़े में बदल देता है, उसी प्रकार कबीर का सुझाव है कि अपनी साधना और अंतर्दृष्टि के माध्यम से, उसने अपना अस्तित्व बदल लिया है।
ममिता मेरा क्या करै, प्रेम उघाड़ी पौलि।
दरसन भया दयाल का, सूल भई सुख सौड़ि॥48॥
इस दोहे में, कबीर गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि व्यक्त करने के लिए मधुमक्खी और सुई के रूपक का उपयोग करते हैं। मधुमक्खी को अक्सर गुरु या प्रिय का प्रतिनिधित्व करने के लिए रूपक के रूप में उपयोग किया जाता है, जबकि सुई साधक या शिष्य का प्रतिनिधित्व करती है।
कबीर मधुमक्खी (गुरु या प्रिय) द्वारा उसे पहुंचाए जाने वाले किसी भी नुकसान की महत्वहीनता पर विचार करते हैं। इसके बजाय, वह प्रिय की उपस्थिति के माध्यम से प्रेम और दिव्य कृपा की रिहाई का अनुभव करता है। मधुमक्खी का प्रतीक यह प्रेम कबीर के हृदय को भर देता है और उन्हें सुई में धागा डालने जैसे अपने कर्तव्य निभाने में सक्षम बनाता है।
इसके अलावा, कबीर ईश्वरीय कृपा की परिवर्तनकारी शक्ति का वर्णन करते हैं। दयालु (प्रिय) के दर्शन या दर्शन से, कबीर के हृदय की सुई पिन की तरह हो जाती है, जो छोटी या महत्वहीन होने की स्थिति का प्रतीक है। विनम्रता और समर्पण की इस स्थिति में, कबीर को सच्चा आनंद और संतुष्टि मिलती है।
साखी – रस कौ अंग
कबीर हरि रस यौं पिया बाकी रही न थाकि।
पाका कलस कुँभार का, बहुरि न चढ़हिं चाकि॥1॥
राम रसाइन प्रेम रस पीवत, अधिक रसाल।
कबीर पीवण दुलभ है, माँगै सीस कलाल॥2॥
कबीर भाठी कलाल की, बहुतक बैठे आइ।
सिर सौंपे सोई पिवै, नहीं तो पिया न जाइ॥3॥
हरि रस पीया जाँणिये, जे कबहूँ न जाइ खुमार।
मैंमंता घूँमत रहै, नाँही तन की सार॥4॥
मैंमंता तिण नां चरै, सालै चिता सनेह।
बारि जु बाँध्या प्रेम कै, डारि रह्या सिरि षेह॥5॥
मैंमंता अविगत रहा, अकलप आसा जीति।
राम अमलि माता रहै, जीवन मुकति अतीकि॥6॥
जिहि सर घड़ा न डूबता, अब मैं गल मलि न्हाइ।
देवल बूड़ा कलस सूँ, पंषि तिसाई जाइ॥7॥
सबै रसाइण मैं किया, हरि सा और न कोइ।
तिल इक घट मैं संचरे, तौ सब तन कंचन होइ॥8
साखी – जर्णा कौ अंग
भारी कहौं त बहु डरौ, हलका कहूँ तो झूठ।
मैं का जाँणौं राम कूं, नैनूं कबहुं न दीठ॥1॥
दीठा है तो कस कहूँ, कह्या न को पतियाइ।
हरि जैसा है तैसा रहौ, तूं हरिषि हरिषि गुण गाइ॥2॥
ऐसा अद्भूत जिनि कथै, अद्भुत राखि लुकाइ
बेद कुरानों गमि नहीं, कह्याँ न को पतियाइ॥3॥
करता की गति अगम है, तूँ चलि अपणैं उनमान।
धीरैं धीरैं पाव दे, पहुँचैगे परवान॥4॥
पहुँचैगे तब कहैंगे, अमड़ैगे उस ठाँइ।
अजहूँ बेरा समंद मैं, बोलि बिगूचै काँइ॥5॥
साखी – लै कौ अंग
जिहि बन सोह न संचरै, पंषि उड़ै नहिं जाइ।
रैनि दिवस का गमि नहीं, तहां कबीर रह्या ल्यो आइ॥1॥
सुरति ढीकुली ले जल्यो, मन नित ढोलन हार।
कँवल कुवाँ मैं प्रेम रस, पीवै बारंबार॥2॥
गंग जमुन उर अंतरै, सहज सुंनि ल्यौ घाट।
तहाँ कबीरै मठ रच्या, मुनि जन जोवैं बाट॥3॥
साखी – निहकर्मी पतिब्रता कौ अंग
कबीर प्रीतडी तौ तुझ सौं, बहु गुणियाले कंत।
जे हँसि बोलौं और सौं, तौं नील रँगाउँ दंत॥1॥
नैना अंतरि आव तूँ, ज्यूँ हौं नैन झँपेउँ।
नाँ हौं देखौं और कूं, नाँ तुझ देखन देउँ॥2॥
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा।
तेरा तुझको सौंपता, क्या लागै है मेरा॥3॥
कबीर रेख स्यंदूर की, काजल दिया न जाइ।
नैनूं रमइया रमि रह्या, दूजा कहाँ समाइ॥4॥
कबीर सीप समंद की, रटै पियास पियास।
संमदहि तिणका बरि गिणै स्वाँति बूँद की आस॥5॥
कबीर सुख कौ जाइ था, आगै आया दुख।
जाहि सुख घरि आपणै हम जाणैं अरु दुख॥6॥
दो जग तो हम अंगिया, यहु डर नाहीं मुझ।
भिस्त न मेरे चाहिये, बाझ पियारे तुझ॥7॥
जे वो एकै न जाँणियाँ तो जाँण्याँ सब जाँण।
जो वो एक न जाँणियाँ, तो सबहीं जाँण अजाँण॥8॥
कबीर एक न जाँणियाँ, तो बहु जाँण्याँ क्या होइ।
एक तैं सब होत है, सब तैं एक न होइ॥9॥
जब लगि भगति सकांमता, तब लग निर्फल सेव।
कहै कबीर वै क्यूं मिलैं, निहकामी निज देव॥10॥
आसा एक जू राम की, दूजी आस निरास।
पाँणी माँहै घर करैं, ते भी मरै पियास॥11॥
आसा एक ज राम की, दूजी आस निवारी।
आसा फिरि फिर मारसी, ज्यूँ चौपड़ि का सारि॥11॥
आसा एक ज राम की जुग जुग पुरवे आस।
जै पाडल क्यों रे करै, बसैहिं जु चंदन पास॥12॥
जे मन लागै एक सूँ, तो निरबाल्या जाइ।
तूरा दुइ मुखि बाजणाँ न्याइ तमाचे खाइ॥12॥
कबीर कलिजुग आइ करि, कीये बहुतज मीत।
जिन दिल बँधी एक सूँ, ते सुखु सोवै नचींत॥13॥
कबीर कुता राम का, मुतिया मेरा नाउँ।
गलै राम की जेवडी, जित खैचे तित जाउँ॥14॥
तो तो करै त बाहुड़ों, दुरि दुरि करै तो जाउँ।
ज्यूँ हरि राखैं त्यूँ रहौं, जो देवै सो खाउँ॥15॥
मन प्रतीति न प्रेम रस, नां इस तन मैं ढंग।
क्या जाणौं उस पीव सूं, कैसे रहसी रंग॥16॥
उस संम्रथ का दास हौं, कदे न होइ अकाज।
पतिब्रता नाँगी रहै, तो उसही पुरिस कौ लाज॥17॥
धरि परमेसुर पाँहुणाँ, सुणौं सनेही दास।
षट रस भोजन भगति करि, ज्यूँ कदे न छाड़ैपास॥18
साखी – चितावणी कौ अंग
कबीर नौबति आपणी, दिन दस लेहु बजाइ।
ए पुर पटन ए गली, बहुरि न देखै आइ॥1॥
जिनके नौबति बाजती, मैंगल बँधते बारि।
एकै हरि के नाँव बिन, गए जन्म सब हारि॥2॥
ढोल दमामा दड़बड़ी, सहनाई संगि भेरि।
औसर चल्या बजाइ करि, है कोइ राखै फेरि॥3॥
सातो सबद जु बाजते, घरि घरि होते राग।
ते मंदिर खाली पड़े, बैसण लागे काग॥4॥
कबीर थोड़ा जीवणा माड़े बहुत मँडाण।
सबही ऊभा मेल्हि गया, राव रंक सुलितान॥5॥
इक दिन ऐसा होइगा, सब सूँ पड़ै बिछोइ।
राजा राणा छत्रापति, सावधान किन होइ॥6॥
ऊजड़ खेड़ै ठीकरी, घड़ि घड़ि गए कुँभार।
रावण सरीखे चलि गए, लंका के सिकदार॥7॥
कबीर पटल कारिवाँ, पंच चोर दस द्वार।
जन राँणौं गढ़ भेलिसी, सुमिरि लै करतार॥7॥
कबीर कहा गरबियौ, इस जीवन की आस।
टेसू फूले दिवस चारि, खंखर भये पलास॥8॥
कबीर कहा गरबियो, देही देखि सुरंग।
बिछड़ियाँ मिलिनौ नहीं, ज्यूँ काँचली भुवंग॥9॥
कबीर कहा गरिबियो, ऊँचे देखि अवास।
काल्हि पर्यूँ भ्वै लेटणाँ, ऊपरि जामैं घास॥10॥
कबीर कहा गरबियौ, चाँम लपेटे हड।
हैबर ऊपरि छत्रा सिरि, ते भी देबा खड॥11॥
कबीर कहा गरबियो, काल गहै कर केस।
नां जाँणों कहाँ मारिसी, कै घरि कै परदेस॥12॥
यहु ऐसा संसार है जैसा सैबल फूल।
दिन दस के व्योहार को, झूठै रंगि न भूल॥13॥
मीति बिसारी बाबरे, अचिरज कीया कौन।
तन माटी में मिलि गया, ज्यूँ आटे मैं लूण॥15॥
जाँभण मरण बिचारि करि, कूडे काँम निहारि।
जिनि पंथू तुझ चालणां, सोई पंथ सँवारि॥14॥
बिन रखवाले बहिरा, चिड़ियैं खाया खेत।
आधा प्रधा ऊबरै, चेति कै तो चेति॥15॥
हाड़ जलै ज्यूँ लाकड़ी, केस जलै ज्यूँ घास।
सब तन जलता देखि करि, भया कबीर उदास॥16॥
मड़ा जलै लकड़ी जलै, जलै जलावणहार।
कौतिगहारे भी जलैं, कासनि करौ पुकार॥23॥
कबीर देवल हाड का, मारी तणा बधाँण।
खड हडता पाया नहीं, देवल का रहनाँण॥24॥
कबीर मंदिर ढहि पड़ा, सेंट भई सैबार।
कोई मंदिर चिणि गया, मिल्या न दूजी बार॥17॥
आजि कि काल्हि कि पचे दिन, जंगल होइगा बास।
ऊपरि ऊपरि फिरहिंगे, ढोर चरंदे घास॥18॥
मरहिंगे मरि जाहिंगे, नांव न लेखा कोइ।
ऊजड़ जाइ बसाहिंगे, छाँड़ि बसंती लोइ॥19॥
कबीर खेति किसाण का, भ्रगौ खाया खाड़ि।
खेत बिचारा क्या करे, जो खसम न करई बाड़ि॥20॥
कबीर देवल ढहि पड़ा, ईंट भई सैवार।
करि चेजारा सौ प्रीतिड़ी, ज्यौं ढहै न दूजी बार॥18॥
कबीर मंदिर लाष का, जड़िया हीरै लालि।
दिवस चारि का पेषणां, विनस जाइगा काल्हि॥19॥
कबीर धूलि सकेलि करि, पुड़ी ज बाँधी एह।
दिवस चारि का पेषणाँ, अंति षेह का षेह॥20॥
कबीर जे धंधै तौ धूलि, बिन धंधे धूलै नहीं।
ते नर बिनठे मूलि, जिनि धंधे मैं ध्याया नहीं॥21॥
कबीर सुपनै रैनि कै, ऊघड़ि आयै नैन।
जीव पड्या बहु लूटि मैं, जागै तो लैण न दैण॥22॥
*टिप्पणी: *ख- बहु भूलि मैं।
कबीर सुपनै रैनि के, पारस जीय मैं छेक।
जे सोऊँ तो दोइ जणाँ, जे जागूँ तो एक॥23॥
कबीर इहै चितावणी, जिन संसारी जाइ।
जे पहिली सुख भोगिया, तिन का गूड ले खाइ॥30॥
कबीर इस संसार में घणै मनिप मतिहींण।
राम नाम जाँणौं नहीं, आये टापी दीन॥24॥
पीपल रूनों फूल बिन, फलबिन रूनी गाइ।
एकाँ एकाँ माणसाँ, टापा दीन्हा आइ॥32॥
कहा कियौ हम आइ करि, कहा करेंगे जाइ।
इत के भए न उत के, चाले मूल गँवाइ॥25॥
आया अणआया भया, जे बहुरता संसार।
पड़ा भुलाँवा गफिलाँ, गये कुबंधी हारि॥26॥
कबीर हरि की भगति बिन, धिगि जीमण संसार।
धूँवाँ केरा धौलहर जात न लागै वार॥27॥
जिहि हरि की चोरी करि, गये राम गुण भूलि।
ते बिंधना बागुल रचे, रहे अरध मुखि झूलि॥28॥
माटी मलणि कुँभार की, घड़ीं सहै सिरि लात।
इहि औसरि चेत्या नहीं, चूका अबकी घात॥29॥
इहि औसरि चेत्या नहीं, पसु ज्यूँ पाली देह।
राम नाम जाण्या नहीं, अति पड़ी मुख षेह्ड्ड30॥
राम नाम जाण्यो नहीं, लानी मोटी षोड़ि।
काया हाँडी काठ की, ना ऊ चढ़े बहोड़ि॥31॥
राम नाम जाण्या नहीं, बात बिनंठी मूलि।
हरत इहाँ ही हारिया, परति पड़ी मुख धूलि॥32॥
राम नाम जाण्या नहीं, मेल्या मनहिं बिसारि।
ते नर हाली बादरी, सदा परा पराए बारि॥42॥
राम नाम जाण्या नहीं, ता मुखि आनहिं आन।
कै मूसा कै कातरा, खाता गया जनम॥43॥
राम नाम जाण्यो नहीं हूवा बहुत अकाज।
बूडा लौरे बापुड़ा बड़ा बूटा की लाज॥44॥
राम नाम जाँण्याँ नहीं, पल्यो कटक कुटुम्ब।
धंधा ही में मरि गया, बाहर हुई न बंब॥33॥
मनिषा जनम दुर्लभ है, देह न बारम्बार।
तरवर थैं फल झड़ि पड़ा बहुरि न लागै डार॥34॥
कबीर हरि की भगति करि, तजि बिषिया रस चोज।
बारबार नहीं पाइए, मनिषा जन्म की मौज॥35॥
पाणी ज्यौर तालाब का दह दिसी गया बिलाइ।
यह सब योंही जायगा, सकै तो ठाहर लाइ॥48॥
कबीर यहु तन जात है, सकै तो ठाहर लाइ।
कै सेवा करि साध की, कै गुण गोविंद के गाइ॥36॥
*टिप्पणी: *ख-के गोबिंद गुण गाइ।
कबीर यह तन जात है, सकै तो लेहु बहोड़ि।
नागे हाथूँ ते गए, जिनके लाख करोड़ि॥37॥
यह तनु काचा कुंभ है, चोट चहूँ दिसि खाइ।
एक राम के नाँव बिन, जदि तदि प्रलै जाइ॥38॥
यह तन काचा कुंभ है, मांहि कया ढिंग बास।
कबीर नैंण निहारियाँ, तो नहीं जीवन आस॥52॥
यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरै था साथि।
ढबका लागा फुटि गया, कछू न आया हाथि॥39॥
काँची कारी जिनि करै, दिन दिन बधै बियाधि।
राम कबीरै रुचि भई, याही ओषदि साधि॥40॥
कबीर अपने जीवतै, ए दोइ बातैं धोइ।
लोग बड़ाई कारणै, अछता मूल न खोइ॥41॥
खंभा एक गइंद दोइ, क्यूँ करि बंधिसि बारि।
मानि करै तो पीव नहीं, पीव तौ मानि निवारि॥42॥
दीन गँवाया दुनी सौं, दुनी न चाली साथि।
पाइ कुहाड़ा मारिया, गाफिल अपणै हाथि॥43॥
यह तन तो सब बन भया, करम भए कुहाड़ि।
आप आप कूँ काटिहैं, कहैं कबीर विचारि॥44॥
कुल खोया कुल ऊबरै, कुल राख्यो कुल जाइ।
राम निकुल कुल भेंटि लैं, सब कुल रह्या समाइ॥45॥
दुनिया के धोखे मुवा, चलै जु कुल की काँण।
तबकुल किसका लाजसी, जब ले धर्या मसाँणि॥46॥
दुनियाँ भाँडा दुख का भरी मुँहामुह भूष।
अदया अलह राम की, कुरलै ऊँणी कूष॥47॥
दुनियां के मैं कुछ नहीं, मेरे दुनी अकथ।
साहिब दरि देखौं खड़ा, सब दुनियां दोजग जंत॥61॥
जिहि जेबड़ी जग बंधिया, तूँ जिनि बँधै कबीर।
ह्नैसी आटा लूँण ज्यूँ, सोना सँवाँ शरीर॥48॥
कहत सुनत जग जात है, विषै न सूझै काल।
कबीर प्यालै प्रेम कै, भरि भरि पिवै रसाल॥49॥
कबीर हद के जीव सूँ, हित करि मुखाँ न बोलि
जे लागे बेहद सूँ, तिन सूँ अंतर खोलि॥50॥
कबीर साषत की सभा, तू मत बैठे जाइ।
एकै बाड़ै क्यू बड़ै, रीझ गदहड़ा गाइ॥65॥
कबीर केवल राम की, तूँ जिनि छाड़ै ओट।
घण अहरणि बिचि लोह ज्यूँ, घड़ी सहे सिर चोट॥51॥
कबीर केवल राम कहि, सुध गरीबी झालि।
कूड़ बड़ाई बूड़सी, भारी पड़सी काल्हि॥52॥
काया मंजन क्या करै, कपड़ धोइम धोइ।
उजल हूवा न छूटिए, सुख नींदड़ी न सोह॥53॥
उजल कपड़ा पहरि करि, पान सुपारी खाँहि।
एके हरि का नाँव बिन, बाँधे जमपुरि जाँहि॥54॥
थली चरंतै म्रिघ लै, बीध्या एक ज सौंण।
हम तो पंथी पंथ सिरि, हर्या चरैगा कौण॥74॥
तेरा संगी कोइ नहीं, सब स्वारथ बँधी लोइ।
मनि परतीति न ऊपजै, जीव बेसास न होइ॥55॥
मांइ बिड़ाणों बाप बिड़, हम भी मंझि बिड़ाह।
दरिया केरी नाव ज्यूँ, संजोगे मिलियाँह॥56॥
इत प्रधर उत घर बड़जण आए हाट।
करम किराणाँ बेचि करि, उठि ज लागे बाट॥57॥
नान्हाँ काती चित दे, महँगे मोलि बिकाइ।
गाहक राजा राम है और न नेड़ा आइ॥58॥
डागल उपरि दौड़णां, सुख नींदड़ी न सोइ।
पुनै पाए द्यौंहणे, ओछी ठौर न खोइ॥59॥
ज्यूँ कोली पेताँ बुणै, बुणतां आवै बोड़ि।
ऐसा लेख मीच का, कछु दौड़ि सके तो दौड़ि॥76॥
मैं मैं बड़ी बलाइ है, सके तो निकसी भाजि।
कब लग राखौं हे सखी, रूई पलेटी आगि॥60॥
मैं मैं मेरी जिनि करै, मेरी मूल बिनास।
मेरी पग का पैषड़ा, मेरी गल की पास॥61॥
मेरे तेर की जीवणी, बसि बंध्या संसार।
कहाँ सुकुँणबा सुत कलित, दाक्षणि बारंबार॥79॥
मेरे तेरे की रासड़ी, बलि बंध्या संसार।
दास कबीरा किमि बँधै, जाकैं राम अधार॥82॥
कबीर नांव जरजरी, भरी बिराणै भारि।
खेवट सौं परचा नहीं, क्यो करि उतरैं पारि॥83॥
कबीर नाव जरजरी, कूड़े खेवणहार।
हलके हलके तिरि गए, बूड़े तिनि सिर भार॥62॥
कबीर पगड़ा दूरि है, जिनकै बिचिहै राति।
का जाणौं का होइगा, ऊगवै तैं परभाति॥84॥
साखी – मन कौ अंग
मन कै मते न चालिये, छाड़ि जीव की बाँणि।
ताकू केरे सूत ज्यूँ, उलटि अपूठा आँणि॥1॥
चिंता चिति निबारिए, फिर बूझिए न कोइ।
इंद्री पसर मिटाइए, सहजि मिलैगा सोइ॥2॥
आसा का ईंधन करूँ, मनसा करुँ विभूति।
जोगी फेरी फिल करौं, यों बिनवाँ वै सूति॥3॥
कबीर सेरी साँकड़ी चंचल मनवाँ चोर।
गुण गावै लैलीन होइ, कछू एक मन मैं और॥4॥
कबीर मारूँ मन कूँ, टूक टूक ह्नै जाइ।
विष की क्यारी बोई करि, लुणत कहा पछिताइ॥5॥
इस मन कौ बिसमल करौं, दीठा करौं अदीठ।
जै सिर राखौं आपणां, तौ पर सिरिज अंगीठ॥6॥
मन जाणैं सब बात, जाणत ही औगुण करै।
काहे की कुसलात, कर दीपक कूँ बैं पड़ै॥7॥
हिरदा भीतरि आरसी, मुख देषणाँ न जाइ।
मुख तौ तौपरि देखिए, जे मन की दुविधा जाइ॥8॥
कबीर मन मृथा भगा, खेत बिराना खाइ।
सूलाँ करि करि से किसी जब खसम पहूँचे आइ॥9॥
मन को मन मिलता नहीं तौ होता तन का भंग।
अब ह्नै रहु काली कांवली, ज्यौं दूजा चढ़ै न रंग॥10॥
मन दीया मन पाइए, मन बिन मन नहीं होइ।
मन उनमन उस अंड ज्यूँ, खनल अकासाँ जोइ॥9॥
मन गोरख मन गोविंदो, मन हीं औघड़ होइ।
जे मन राखै जतन करि, तौ आपै करता सोइ॥10॥
एक ज दोसत हम किया, जिस गलि लाल कबाइ।
एक जग धोबी धोइ मरै, तौ भी रंग न जाइ॥11॥
पाँणी ही तैं पातला, धूवाँ ही तै झींण।
पवनाँ बेगि उतावला, सो दोसत कबीरै कीन्ह॥12॥
कबीर तुरी पलांड़ियाँ, चाबक लीया हाथि।
दिवस थकाँ साँई मिलौं, पीछे पड़िहै राति।॥13॥
मनवां तो अधर बस्या, बहुतक झीणां होइ।
आलोकत सचु पाइया, कबहूँ न न्यारा सोइ॥14॥
मन न मार्या मन करि, सके न पंच प्रहारि।
सीला साच सरधा नहीं, इंद्री अजहुँ उद्यारि॥15॥
कबीर मन बिकरै पड़ा, गया स्वादि के साथ।
गलका खाया बरज्ताँ, अब क्यूँ आवै हाथि॥16॥
कबीर मन गाफिल भया, सुमिरण लागै नाहिं।
घणीं सहैगा सासनाँ, जम की दरगह माहिं॥17॥
कोटि कर्म पल मैं करै, यहु मन बिषिया स्वादि।
सतगुर सबद न मानई, जनम गँवाया बादि॥18॥
मैंमंता मन मारि रे, घटहीं माँहै घेरि।
जबहीं चालै पीठि दै, अंकुस दे दे फेरि॥19॥
जौ तन काँहै मन धरै, मन धरि निर्मल होइ।
साहिब सौ सनमुख रहै, तौ फिरि बालक होइ॥
मैंमंता मन मारि रे, नान्हाँ करि करि पीसि।
तब सुख पावै सुंदरी, ब्रह्म झलकै सीसि॥20॥
कागद केरी नाँव री, पाँणी केरी गंग।
कहै कबीर कैसे तिरूँ, पंच कुसंगी संग॥21॥
कबीर यह मन कत गया, जो मन होता काल्हि।
डूंगरि बूठा मेह ज्यूँ, गया निबाँणाँ चालि॥22॥
मृतक कूँ धी जौ नहीं, मेरा मन बी है।
बाजै बाव बिकार की, भी मूवा जीवै॥23॥
काटि कूटि मछली, छींकै धरी चहोड़ि।
कोइ एक अषिर मन बस्या, दह मैं पड़ी बहोड़ि॥24॥
मूवा मन हम जीवत, देख्या जैसे मडिहट भूत।
मूवाँ पीछे उठि उठि लागै, ऐसा मेरा पूत॥47॥
मूवै कौंधी गौ नहीं, मन का किया बिनास।
कबीर मन पंषी भया, बहुतक चढ़ा अकास।
उहाँ ही तैं गिरि पड़ा, मन माया के पास॥25॥
भगति दुबारा सकड़ा राई दसवैं भाइ।
मन तौ मैंगल ह्नै रह्यो, क्यूँ करि सकै समाइ॥26॥
करता था तो क्यूँ रह्या, अब करि क्यूँ पछताइ।
बोवै पेड़ बबूल का, अब कहाँ तैं खाइ॥27॥
काया देवल मन धजा, विष्रै लहरि फरराइ।
मन चाल्याँ देवल चलै, ताका सर्बस जाइ॥28॥
मनह मनोरथ छाँड़ि दे, तेरा किया न होइ।
पाँणी मैं घीव गीकसै, तो रूखा खाइ न कोइ॥29॥
काया कसूं कमाण ज्यूँ, पंचतत्त करि बांण।
मारौं तो मन मृग को, नहीं तो मिथ्या जाँण॥30॥
कबीर हरि दिवान कै, क्यूँकर पावै दादि।
पहली बुरा कमाइ करि, पीछे करै फिलादि॥35॥
साखी – सूषिम मारग कौ अंग
कौंण देस कहाँ आइया, कहु क्यूँ जाँण्याँ जाइ।
उहू मार्ग पावै नहीं, भूलि पड़े इस माँहि॥1॥
उतीथैं कोइ न आवई, जाकूँ बूझौं धाइ।
इतथैं सबै पठाइये, भार लदाइ लदाइ॥2॥
*टिप्पणी: *ख में इसके आगे यह दोहा है-
कबीर संसा जीव मैं, कोइ न कहै समुझाइ।
नाँनाँ बांणी बोलता, सो कत गया बिलाइ॥3॥
सबकूँ बूझत मैं फिरौं, रहण कहै नहीं कोइ।
प्रीति न जोड़ी राम सूँ, रहण कहाँ थैं होइ॥3॥
चलो चलौं सबको कहे, मोहि अँदेसा और।
साहिब सूँ पर्चा नहीं, ए जांहिगें किस ठौर॥4॥
जाइबे को जागा नहीं, रहिबे कौं नहीं ठौर।
कहै कबीरा संत हौ, अबिगति की गति और॥5॥
कबीरा मारिग कठिन है, कोइ न सकई जाइ।
गए ते बहुडे़ नहीं, कुसल कहै को आइ॥6॥
जन कबीर का सिषर घर, बाट सलैली सैल।
पाव न टिकै पपीलका, लोगनि लादे बैल॥7॥
जहाँ न चींटी चढ़ि सकै, राइ न ठहराइ।
मन पवन का गमि नहीं, तहाँ पहूँचे जाइ॥8॥
कबीर मारग अगम है, सब मुनिजन बैठे थाकि।
तहाँ कबीरा चलि गया गहि सतगुर कीसाषि॥9॥
सुर न थाके मुनि जनां, जहाँ न कोई जाइ।
मोटे भाग कबीर के, तहाँ रहे घर छाइ॥10॥
साखी – माया कौ अंग
जग हठवाड़ा स्वाद ठग, माया बेसाँ लाइ।
रामचरण नीकाँ गही, जिनि जाइ जनम ठगाइ॥1॥
कबीर जिभ्या स्वाद ते, क्यूँ पल में ले काम।
अंगि अविद्या ऊपजै, जाइ हिरदा मैं राम॥2॥
कबीर माया पापणीं, फंध ले बैठि हाटि।
सब जग तो फंधै पड़ा, गया कबीरा काटि॥2॥
कबीर माया पापणीं, लालै लाया लोंग।
पूरी कीनहूँ न भोगई, इनका इहै बिजोग॥3॥
कबीरा माया पापणीं, हरि सूँ करे हराम।
मुखि कड़ियाली कुमति की, कहण न देईं राम॥4॥
जाँणी जे हरि को भजौ, मो मनि मोटी आस।
हरि बिचि घालै अंतरा, माया बड़ी बिसास॥5॥
कबीर माया मोहनी, मोहे जाँण सुजाँण।
भागाँ ही छूटै नहीं, भरि भरि मारै बाँण॥6॥
कबीर माया मोहनी, जैसी मीठी खाँड़।
सतगुर की कृपा भई, नहीं तो करती भाँड़॥7॥
कबीर माया मोहनी, सब जग घाल्या घाँणि।
कोइ एक जन ऊबरै, जिनि तोड़ी कुल की काँणि॥8॥
कबीर माया मोहनी, माँगी मिलै न हाथि।
मनह उतारी झूठ करि, तब लागी डौलै साथि॥9॥
माया दासी संत की, ऊँभी देइ असीस।
बिलसी अरु लातौं छड़ी सुमरि सुमरि जगदीस॥10॥
माया मुई न मन मुवा, मरि मरि गया सरीर।
आसा त्रिस्नाँ ना मुई, यों कहि गया कबीर॥11॥
आसा जीवै जग मरै, लोग मरे मरि जाइ।
सोइ मूबे धन संचते, सो उबरे जे खाइ॥12॥
कबीर सो धन संचिए, जो आगै कूँ होइ।
सीस चढ़ाए पोटली, ले जात न देख्या कोइ॥13॥
त्रीया त्रिण्णाँ पापणी, तासूँ प्रीति न जोड़ि।
पैड़ी चढ़ि पाछाँ पड़े, लागै मोटी खोड़ि॥14॥
त्रिष्णाँ सींची नाँ बुझे, दिन दिन बढ़ती जाइ।
जबासा के रूप ज्यूँ, घण मेहाँ कुमिलाइ॥15॥
कबीर जग की को कहे, भौ जलि बूड़ै दास।
पारब्रह्म पति छाड़ि कर, करैं मानि की आस॥16॥
माया तजी तौ का भया, मानि तजी नहीं जाइ।
मानि बड़े गुनियर मिले, मानि सबनि की खाइ॥17॥
रामहिं थोड़ा जाँणि करि, दुनियाँ आगैं दीन।
जीवाँ कौ राजा कहै, माया के आधीन॥18॥
रज बीरज की कली, तापरि साज्या रूप।
राम नाम बिन बूड़ि है, कनक काँमणी कूप॥19॥
माया तरवर त्रिविध का, साखा दुख संताप।
सीतलता सुपिनै नहीं, फल फीको तनि ताप॥20॥
कबीर माया ढाकड़ी, सब किसही कौ खाइ।
दाँत उपाणौं पापड़ी, जे संतौं नेड़ी जाइ॥21॥
नलनी सायर घर किया, दौं लागी बहुतेणि।
जलही माँहै जलि मुई, पूरब जनम लिपेणि॥22॥
कबीर गुण की बादली, ती तरबानी छाँहिं।
बाहरि रहे ते ऊबरे, भीगें मंदिर माँहिं॥23॥
कबीर माया मोह की, भई अँधारी लोइ।
जे सूते ते मुसि लिये, रहे बसत कूँ रोइ॥24॥
माया काल की खाँणि है, धरि त्रिगणी बपरौति।
जहाँ जाइ तहाँ सुख नहीं, यह माया की रीति॥
संकल ही तैं सब लहे, माया इहि संसार।
ते क्यूँ छूटे बापुड़े, बाँधे सिरजनहार॥25॥
बाड़ि चढ़ती बेलि ज्यूँ, उलझी, आसा फंध।
तूटै पणि छूटै नहीं, भई ज बाना बंध॥26॥
सब आसण आस तणाँ, त्रिबर्तिकै को नाहिं।
थिवरिति कै निबहै नहीं, परिवर्ति परपंच माँहि॥27॥
कबीर इस संसार का, झूठा माया मोह।
जिहि घरि जिता बधावणाँ, तिहि घरि तिता अँदोह॥28॥
माया हमगौ यों कह्या, तू मति दे रे पूठि।
और हमारा हम बलू गया कबीरा रूठि॥29॥
बुगली नीर बिटालिया, सायर चढ़ा कलंक।
और पँखेरू पी गए, हंस न बोवै चंच॥30॥
कबीर माया जिनि मिलैं, सो बरियाँ दे बाँह।
नारद से मुनियर मिले, किसौ भरोसे त्याँह॥31॥
माया की झल जग जल्या, कनक काँमणीं लागि।
कहुँ धौं किहि विधि राखिये, रूई पलेटी आगि॥32॥
साखी – चाँणक कौ अंग
जीव बिलव्या जीव सों, अलप न लखिया जाइ।
गोबिंद मिलै न झल बुझै, रही बुझाइ बुझाइ॥1॥
इही उदर के कारणै, जग जाँच्यो निस जाम।
स्वामी पणौ जु सिर चढ़ो, सर्या न एको काम॥2॥
स्वामी हूँणाँ सोहरा, दोद्धा हूँणाँ दास।
गाडर आँणीं ऊन कूँ, बाँधी चरै कपास॥3॥
स्वामी हूवा सीतका, पैका कार पचास।
राम नाँम काँठै रह्या, करै सिषां की आस॥4॥
कबीर तष्टा टोकणीं, लीए फिरै सुभाइ।
रामनाम चीन्हें नहीं, पीतलि ही कै चाइ॥5॥
कलि का स्वामी लोभिया, पीतलि धरी षटाइ।
राज दुबाराँ यौं फिरै, ज्यूँ हरिहाई गाइ॥6॥
कलि का स्वामी लोभिया, मनसा धरी बधाइ।
दैहिं पईसा ब्याज कौं, लेखाँ करताँ जाइ॥7॥
कबीर कलि खोटी भई, मुनियर मिलै न कोइ।
लालच लोभी मसकरा, तिनकूँ आदर होइ॥8॥
चारिउ बेद पढ़ाइ करि, हरि सूँ न लाया हेत।
बालि कबीरा ले गया, पंडित ढूँढ़ै खेत॥9॥
बाँम्हण गुरु जगत का, साधू का गुरु नाहिं।
उरझि पुरझि करि मरि रह्या, चारिउँ बेदाँ माहिं॥10॥
बाम्हण बूड़ा बापुड़ा, जेनेऊ कै जोरि।
लख चौरासी माँ गेलई, पारब्रह्म सों तोडि॥12॥)
साषित सण का जेवणा, भीगाँ सूँ कठठाइ।
दोइ अषिर गुरु बाहिरा, बाँध्या जमपुरि जाइ॥11॥
कबीर साषत की सभा, तूँ जिनि बैसे जाइं।
एक दिबाड़ै क्यूँ बडै, रीझ गदेहड़ा गाइ॥14॥
साषत ते सूकर भला, सूचा राखे गाँव।
बूड़ा साषत बापुड़ा, बैसि समरणी नाँव॥15॥
साषत बाम्हण जिनि मिलैं, बैसनी मिलौ चंडाल।
अंक माल दे भेटिए, मानूँ मिले गोपाल॥16॥)
पाड़ोसी सू रूसणाँ, तिल तिल सुख की हाँणि।
पंडित भए सरावगी, पाँणी पीवें छाँणि॥12॥
पंडित सेती कहि रह्या, भीतरि भेद्या नाहिं।
औरूँ कौ परमोधतां, गया मुहरकाँ माँहि॥13॥
चतुराई सूवै पढ़ी, सोई पंजर माँहि।
फिरि प्रमोधै आन कौ, आपण समझै नाहिं॥14॥
रासि पराई राषताँ, खाया घर का खेत।
औरौं कौ प्रमोधतां, मुख मैं पड़िया रेत॥15॥
कबीर कहै पोर कुँ, तूँ समझावै सब कोइ।
संसा पड़गा आपको, तौ और कहे का होइ॥21॥)
तारा मंडल बैसि करि, चंद बड़ाई खाइ।
उदै भया जब सूर का, स्यूँ ताराँ छिपि जाइ॥16॥
देषण के सबको भले, जिसे सीत के कोट।
रवि के उदै न दीसहीं, बँधे न जल की पोट॥17॥
सुणत सुणावत दिन गए, उलझि न सुलझा मान।
कहै कबीर चेत्यौ नहीं, अजहुँ पहलौ दिन॥24॥)
तीरथ करि करि जग मुवा, डूँधै पाँणी न्हाइ।
राँमहि राम जपंतड़ाँ, काल घसीट्याँ जाइ॥18॥
कासी काँठै घर करैं, पीवैं निर्मल नीर।
मुकति नहीं हरि नाँव बिन, यों कहें दास कबीर॥19॥
कबीर इस संसार को, समझाऊँ कै बार।
पूँछ जु पकड़ै भेड़ की, उतर्या चाहै पार॥20॥
पद गायाँ मन हरषियाँ, साषी कह्यां आनंद।
सो तत नाँव न जाणियाँ, गल मैं पड़ि गया फंद॥)
कबीर मन फूल्या फिरै, करता हूँ मैं ध्रंम।
कोटि क्रम सिरि ले चल्या, चेत न देखै भ्रंम॥21॥
मोर तोर की जेवड़ी, बलि बंध्या संसार।
काँ सिकडूँ बासुत कलित, दाझड़ बारंबार॥22॥
साखी – साँच कौ अंग
कबीर पूँजी साह की, तूँ जिनि खोवै ष्वार।
खरी बिगूचनि होइगी, लेखा देती बार॥1॥
लेखा देणाँ सोहरा, जे दिल साँचा होइ।
उस चंगे दीवाँन मैं, पला न पकड़े कोइ॥2॥
कबीर चित्त चमंकिया, किया पयाना दूरि।
काइथि कागद काढ़िया, तब दरिगह लेखा पूरि॥3॥
काइथि कागद काढ़ियां, तब लेखैं वार न पार।
जब लग साँस सरीर मैं, तब लग राम सँभार॥4॥
यहु सब झूठी बंदिगी, बरियाँ पंच निवाज।
साचै मारै झूठ पढ़ि, काजी करै अकाज॥5॥
कबीर काजी स्वादि बसि, ब्रह्म हतै तब दोइ।
चढ़ि मसीति एकै कहै, दरि क्यूँ साचा होइ॥6॥
काजी मुलाँ भ्रमियाँ, चल्या दुनीं कै साथि।
दिल थैं दीन बिसारिया, करद लई जब हाथि॥7॥
जोरी कलिर जिहै करै, कहते हैं ज हलाल।
जब दफतर देखंगा दई, तब हैगा कौंण हवाल॥8॥
जोरी कीयाँ जुलम है, माँगे न्याव खुदाइ।
खालिक दरि खूनी खड़ा, मार मुहे मुहि खाइ॥9॥
साँई सेती चोरियाँ, चोराँ सेती गुझ।
जाँणैगा रे जीवड़ा, मर पड़ैगी तुझ॥10॥
सेष सबूरी बाहिरा, क्या हज काबैं जाइ।
जिनकी दिल स्याबति नहीं, तिनकौं कहाँ खुदाइ॥11॥
खूब खाँड है खोपड़ी, माँहि पड़ै दुक लूँण।
पेड़ा रोटी खाइ करि, गला कटावै कौंण॥12॥
पापी पूजा बैसि करि, भषै माँस मद दोइ।
तिनकी दष्या मुकति नहीं, कोटि नरक फल होइ॥13॥
सकल बरण इकत्रा है, सकति पूजि मिलि खाँहिं।
हरि दासनि की भ्रांति करि, केवल जमपुरि जाँहिं॥14॥
कबीर लज्या लोक की, सुमिरै नाँही साच।
जानि बूझि कंचन तजै, काठा पकड़े काच॥15॥
कबीर जिनि जिनि जाँणियाँ, करत केवल सार।
सो प्राणी काहै चलै, झूठे जग की लार॥16॥
झूठे को झूठा मिलै, दूणाँ बधै सनेह।
झूठे कूँ साचा मिलै, तब ही तूटै नेह॥17॥
साखी – भ्रम विधौंसण कौ अंग
पांहण केरा पूतला, करि पूजै करतार।
इही भरोसै जे रहे, ते बूड़े काली धार॥1॥
काजल केरी कोठरी, मसि के कर्म कपाट।
पांहनि बोई पृथमी, पंडित पाड़ी बाट॥2॥
पाँहिन फूँका पूजिए, जे जनम न देई जाब।
आँधा नर आसामुषी, यौंही खोवै आब॥3॥
कबीर गुड कौ गमि नहीं, पाँषण दिया बनाइ।
सिष सोधी बिन सेविया, पारि न पहुँच्या जाइ॥5॥)
हम भी पाहन पूजते, होते रन के रोझ।
सतगुर की कृपा भई, डार्या सिर थैं बोझ॥4॥
जेती देषौं आत्मा, तेता सालिगराँम।
साथू प्रतषि देव हैं, नहीं पाथर सू काँम॥5॥
कबीर माला काठ की, मेल्ही मुगधि झुलाइ।
सुमिरण की सोधी नहीं, जाँणै डीगरि घाली जाइ॥6॥)
सेवैं सालिगराँम कूँ, मन की भ्रांति न जाइ।
सीतलता सुषिनै नहीं, दिन दिन अधकी लाइ॥6॥
माला फेरत जुग भया, पाय न मन का फेर।
कर का मन का छाँड़ि दे, मन का मन का फेर॥8॥)
सेवैं सालिगराँम कूँ, माया सेती हेत।
बोढ़े काला कापड़ा, नाँव धरावैं सेत॥7॥
जप तप दीसै थोथरा, तीरथ ब्रत बेसास।
सूवै सैबल सेविया, यों जग चल्या निरास॥8॥
तीरथ त सब बेलड़ी, सब जग मेल्या छाइ।
कबीर मूल निकंदिया, कोण हलाहल खाइ॥9॥
मन मथुरा दिल द्वारिका, काया कासी जाँणि।
दसवाँ द्वारा देहुरा, तामै जोति पिछाँणि॥10॥
कबीर दुनियाँ देहुरै, सोस नवाँवण जाइ।
हिरदा भीतर हरि बसै, तूँ ताही सौ ल्यौ लाइ॥11॥
साखी – भेष कौ अंग
कर सेती माला जपै, हिरदै बहै डंडूल।
पग तौ पाला मैं गिल्या, भाजण लागी सूल॥1॥
कर पकरै अँगुरी गिनै, मन धावै चहुँ वीर।
जाहि फिराँयाँ हरि मिलै, सो भया काठ की ठौर॥2॥
माला पहरैं मनमुषी, ताथैं कछु न होइ।
मन माला कौं फेरताँ, जुग उजियारा सोइ॥3॥
माला पहरे मनमुषी, बहुतैं फिरै अचेत।
गाँगी रोले बहि गया, हरि सूँ नाँहीं हेत॥4॥
कबीर माला काठ की, कहि समझावै तोहि।
मन न फिरावै आपणों, कहा फिरावै मोहि॥5॥
कबीर माला मन की, और संसारी भेष।
माला पहर्या हरि मिलै, तौ अरहट कै गलि देष॥6॥
माला पहर्याँ कुछ नहीं, रुल्य मूवा इहि भारि।
बाहरि ढोल्या हींगलू भीतरि भरी भँगारि॥7॥
माला पहर्याँ कुछ नहीं, काती मन कै साथि।
जब लग हरि प्रकटै नहीं, तब लग पड़ता हाथि॥8॥
माला पहर्याँ कुछ नहीं, गाँठि हिरदा की खोइ।
हरि चरनूँ चित्त राखिये, तौ अमरापुर होइ॥9॥
माला पहर्याँ कुछ नहीं बाम्हण भगत न जाण।
ब्याँह सराँधाँ कारटाँ उँभू वैंसे ताणि॥2॥)
माला पहर्या कुछ नहीं, भगति न आई हाथि।
माथौ मूँछ मुँड़ाइ करि, चल्या जगत कै साथि॥10॥
साँईं सेती साँच चलि, औराँ सूँ सुध भाइ।
भावै लम्बे केस करि, भावै घुरड़ि मुड़ाइ॥11॥
केसौं कहा बिगाड़िया, जे मूड़े सौ बार।
मन कौं न काहे मूड़िए, जामै बिषै विकार॥12॥
मन मेवासी मूँड़ि ले, केसौं मूड़े काँइ।
जे कुछ किया सु मन किया, केसौं कीया नाँहि॥13॥
मूँड़ मुँड़ावत दिन गए, अजहूँ न मिलिया राम
राँम नाम कहु क्या करैं, जे मन के औरे काँम॥14॥
स्वाँग पहरि सोरहा भया, खाया पीया षूँदि।
जिहि सेरी साधू नीकले, सो तौ मेल्ही मूँदि॥15॥
बेसनों भया तौ क्या भया, बूझा नहीं बबेक।
छापा तिलक बनाइ करि, दगध्या लोक अनेक॥16॥
तन कौं जोगी सब करैं, मन कों बिरला कोइ।
सब सिधि सहजै पाइए, जे मन जोगी होइ॥17॥
कबीर यहु तौ एक है, पड़दा दीया भेष।
भरम करम सब दूरि करि, सबहीं माँहि अलेष॥18॥
भरम न भागा जीव का, अनंतहि धरिया भेष।
सतगुर परचे बाहिरा, अंतरि रह्या अलेष॥19॥
जगत जहंदम राचिया, झूठे कुल की लाज।
तन बिनसे कुल बिनसि है, गह्या न राँम जिहाज॥20॥
पष ले बूडी पृथमीं, झूठी कुल की लार।
अलष बिसारौं भेष मैं, बूड़े काली धार॥21॥
चतुराई हरि नाँ मिले, ऐ बाताँ की बात।
एक निसप्रेही निरधार का, गाहक गोपीनाथ॥22॥
नवसत साजे काँमनीं, तन मन रही सँजोइ।
पीव कै मन भावे नहीं, पटम कीयें क्या होइ॥23॥
जब लग पीव परचा नहीं, कन्याँ कँवारी जाँणि।
हथलेवा होसै लिया, मुसकल पड़ी पिछाँणि॥24॥
कबीर हरि की भगति का, मन मैं परा उल्लास।
मैं वासा भाजै नहीं, हूँण मतै निज दास॥25॥
मैं वासा मोई किया, दुरिजिन काढ़े दूरि।
राज पियारे राँम का, नगर बस्या भरिपूरि॥26॥
साखी – साध कौ अंग
कबीर संगति साध की, कदे न निरफल होइ।
चंदन होसी बाँवना, नीब न कहसी कोइ॥1॥
कबीर संगति साध की, बेगि करीजैं जाइ।
दुरमति दूरि गँवाइसी, देसी सुमति बताइ॥2॥
मथुरा जावै द्वारिका, भावैं जावैं जगनाथ।
साध संगति हरि भगति बिन, कछू न आवै हाथ॥3॥
मेरे संगी दोइ जणाँ एक बैष्णों एक राँम।
वो है दाता मुकति का, वो सुमिरावै नाँम॥4॥
कबीरा बन बन में फिरा, कारणि अपणें राँम।
राम सरीखे जन मिले, तिन सारे सब काँम॥5॥
कबीर सोई दिन भला, जा दिन संत मिलाहिं।
अंक भरे भरि भेटिया, पाप सरीरौ जाँहिं॥6॥
कबीर चन्दन का बिड़ा, बैठ्या आक पलास।
आप सरीखे करि लिए जे होत उन पास॥7॥
कबीर खाईं कोट की, पांणी पीवे न कोइ
आइ मिलै जब गंग मैं, तब सब गंगोदिक होइ॥8॥
जाँनि बूझि साचहि तजै, करैं झूठ सूँ नेह।
ताको संगति राम जी, सुपिनै हो जिनि देहु॥9॥
कबीर तास मिलाइ, जास हियाली तूँ बसै।
वहि तर वेगि उठाइ, नित को गंजन को सहै॥10॥
केती लहरि समंद की, कत उपजै कत जाइ।
बलिहारी ता दास की, उलटी माँहि समाइ॥11॥
पंच बल धिया फिरि कड़ी, ऊझड़ ऊजड़ि जाइ।
बलिहारी ता दास की, बवकि अणाँवै ठाइ॥12॥
काजल केरी कोठड़ी, तैसा यह संसार।
बलिहारी ता दास की, पैसि जु निकसण हार॥13॥)
काजल केरी कोठढ़ी, काजल ही का कोट।
बलिहारी ता दास की, जे रहै राँम की ओट॥12॥
भगति हजारी कपड़ा, तामें मल न समाइ।
साषित काली काँवली, भावै तहाँ बिछाइ॥13॥
साखी – साध साषीभूत कौ अंग
निरबैरी निहकाँमता, साँई सेती नेह।
विषिया सूँ न्यारा रहै, संतहि का अँग एह॥1॥
संत न छाड़ै संतई, जे कोटिक मिलै असंत।
चंदन भुवंगा बैठिया, तउ सीतलता न तजंत॥2॥
कबीर हरि का भाँवता, दूरैं थैं दीसंत।
तन षीणा मन उनमनाँ, जग रूठड़ा फिरंत॥3॥
कबीर हरि का भावता, झीणाँ पंजर तास।
रैणि न आवै नींदड़ी, अंगि न चढ़ई मास॥4॥
अणरता सुख सोवणाँ, रातै नींद न आइ।
ज्यूँ जल टूटै मंछली यूँ बेलंत बिहाइ॥5॥
जिन्य कुछ जाँण्याँ नहीं तिन्ह, सुख नींदणी बिहाइ।
मैंर अबूझी बूझिया, पूरी पड़ी बलाइ॥6॥
जाँण भगत का नित मरण अणजाँणे का राज।
सर अपसर समझै नहीं, पेट भरण सूँ काज॥7॥
जिहि घटिजाँण बिनाँण है, तिहि घटि आवटणाँ घणाँ।
बिन षंडै संग्राम है नित उठि मन सौं झूमणाँ॥8॥
राम बियोगी तन बिकल, ताहि न चीन्है कोइ।
तंबोली के पान ज्यूँ, दिन दिन पीला होइ॥9॥
पीलक दौड़ी साँइयाँ, लोग कहै पिंड रोग।
छाँनै लंधण नित करै, राँम पियारे जोग॥10॥
काम मिलावै राम कूँ, जे कोई जाँणै राषि।
कबीर बिचारा क्या करे, जाकी सुखदेव बोले साषि॥11॥
काँमणि अंग बिरकत भया, रत भया हरि नाँहि।
साषी गोरखनाथ ज्यूँ, अमर भए कलि माँहि॥12॥
जदि विषै पियारी प्रीति सूँ, तब अंतर हरि नाँहि।
जब अंतर हरि जी बसै, तब विषिया सूँ चित नाँहि॥13॥
जिहि घट मैं संसौ बसै, तिहिं घटि राम न जोइ।
राम सनेही दास विचि, तिणाँ न संचर होइ॥14॥
स्वारथ को सबको सगा, सब सगलाही जाँणि।
बिन स्वारथ आदर करै, सो हरि की प्रीति पिछाँणि॥15॥
जिहिं हिरदै हरि आइया, सो क्यूँ छाँनाँ होइ।
जतन जतन करि दाबिए, तऊ उजाजा सोइ॥16॥
फाटै दीदे मैं फिरौं, नजरि न आवै कोइ।
जिहि घटि मेरा साँइयाँ, सो क्यूँ छाना होइ॥17॥
सब घटि मेरा साँइयाँ, सूनी सेज न कोइ।
भाग तिन्हौ का हे सखी, जिहि घटि परगड होइ॥18॥
पावक रूपी राँम है, घटि घटि रह्या समाइ।
चित चकमक लागै नहीं, ताथैं धुँवाँ ह्नै ह्नै जाइ॥19॥
कबीर खालिक जागिया, और न जागै कोइ।
कै जागै बिसई विष भर्या, कै दास बंदगी होइ॥20॥
कबीर चाल्या जाइ था, आगैं मिल्या खुदाइ।
मीराँ मुझ सौं यौं कह्या, किनि फुरमाई गाइ॥21॥
साखी – मधि कौ अंग
कबीर मधि अंग जेको रहै, तौ तिरत न लागै बार।
दुइ दुइ अंग सूँ लाग करि, डूबत है संसार॥1॥
कबीर दुविधा दूरि करि, एक अंग ह्नै लागि।
यहु सीतल वहु तपति है दोऊ कहिये आगि॥2॥
अनल अकाँसाँ घर किया, मधि निरंतर बास।
बसुधा ब्यौम बिरकत रहै, बिनठा हर बिसवास॥3॥
बासुरि गमि न रैंणि गमि, नाँ सुपनै तरगंम।
कबीर तहाँ बिलंबिया, जहाँ छाहड़ी न घंम॥4॥
जिहि पैडै पंडित गए, दुनिया परी बहीर।
औघट घाटी गुर कही, तिहिं चढ़ि रह्या कबीर॥5॥
श्रग नृकथै हूँ रह्या, सतगुर के प्रसादि।
चरन कँवल की मौज मैं, रहिसूँ अंतिरु आदि॥6॥
हिंदू मूये राम कहि, मुसलमान खुदाइ।
कहै कबीर सो जीवता, दुइ मैं कदे न जाइ॥7॥
दुखिया मूवा दुख कों, सुखिया सुख कौं झूरि।
सदा आनंदी राम के, जिनि सुख दुख मेल्हे दूरि॥8॥
कबीर हरदी पीयरी, चूना ऊजल भाइ।
रामसनेही यूँ मिले, दुन्यूँ बरन गँवाइ॥9॥
काबा फिर कासी भया, राँम भया रहीम।
मोट चून मैदा भया, बैठि कबीरा जीभ॥10॥
धरती अरु आसमान बिचि, दोइ तूँबड़ा अबध।
षट दरसन संसै पड़ा, अरु चौरासी सिध॥11॥
साखी – उपदेश कौ अंग
हरि जी यहै बिचारिया, साषी कहौ कबीर।
भौसागर मैं जीव है, जे कोई पकड़ैं तीर॥1॥
कली काल ततकाल है, बुरा करौ जिनि कोइ।
अनबावै लोहा दाहिणै बोबै सु लुणता होइ॥2॥
जीवन को समझै नहीं, मुबा न कहै संदेस।
जाको तन मन सौं परचा नहीं, ताकौ कौण धरम उपदेस॥3॥)
कबीर संसा जीव मैं, कोई न कहै समझाइ।
बिधि बिधि बाणों बोलता सो कत गया बिलाइ॥3॥
कबीर संसा दूरि करि जाँमण मरण भरंम।
पंचतत तत्तहि मिले सुरति समाना मंन॥4॥
ग्रिही तौ च्यंता घणीं, बैरागी तौ भीष।
दुहुँ कात्याँ बिचि जीव है, दौ हमैं संतौं सीष॥5॥
बैरागी बिरकत भला, गिरहीं चित्त उदार।
दुहै चूकाँ रीता पड़ै, ताकूँ वार न पार॥6॥
जैसी उपजै पेड़ मूँ, तैसी निबहै ओरि।
पैका पैका जोड़ताँ, जुड़िसा लाष करोड़ि॥7॥
कबीर हरि के नाँव सूँ, प्रीति रहै इकतार।
तौ मुख तैं मोती झड़ैं, हीरे अंत न पार॥8॥
ऐसी बाँणी बोलिये, मन का आपा खोइ।
अपना तन सीतल करै, औरन कौं सुख होइ॥9॥
कोइ एक राखै सावधान, चेतनि पहरै जागि।
बस्तन बासन सूँ खिसै, चोर न सकई लागि॥10॥
साखी – बेसास कौ अंग
जिनि नर हरि जठराँह, उदिकै थैं षंड प्रगट कियौ।
सिरजे श्रवण कर चरन, जीव जीभ मुख तास दीयो॥
उरध पाव अरध सीस, बीस पषां इम रषियौ।
अंन पान जहां जरै, तहाँ तैं अनल न चषियौ॥
इहिं भाँति भयानक उद्र में, न कबहू छंछरै।
कृसन कृपाल कबीर कहि, इम प्रतिपालन क्यों करै॥1॥
भूखा भूखा क्या करै, कहा सुनावै लोग।
भांडा घड़ि जिनि मुख दिया, सोई पूरण जोग॥2॥
रचनहार कूँ चीन्हि लै, खैचे कूँ कहा रोइ।
दिल मंदिर मैं पैसि करि, तांणि पछेवड़ा सोइ॥3॥
राम नाम करि बोहड़ा, बांही बीज अधाइ।
अंति कालि सूका पड़ै, तौ निरफल कदे न जाइ॥4॥
च्यंतामणि मन में बसै, सोई चित्त मैं आंणि।
बिन च्यंता च्यंता करै, इहै प्रभू की बांणि॥5॥
कबीर का तूँ चितवै, का तेरा च्यंत्या होइ।
अणच्यंत्या हरिजी करै, जो तोहि च्यंत न होइ॥6॥
करम करीमां लिखि रह्या, अब कछू लिख्या न जाइ।
मासा घट न तिल बथै, जौ कोटिक करै उपाइ॥7॥
जाकौ चेता निरमया, ताकौ तेता होइ।
रती घटै न तिल बधै, जौ सिर कूटै कोइ॥8॥
करीम कबीर जु विह लिख्या, नरसिर भाग अभाग।
जेहूँ च्यंता चितवै, तऊ स आगै आग॥10॥)
च्यंता न करि अच्यंत रहु, सांई है संभ्रथ।
पसु पंषरू जीव जंत, तिनको गांडि किसा ग्रंथ॥9॥
संत न बांधै गाँठड़ी, पेट समाता लेइ।
सांई सूँ सनमुख रहै, जहाँ माँगै तहाँ देइ॥10॥
राँम राँम सूँ दिल मिलि, जन हम पड़ी बिराइ।
मोहि भरोसा इष्ट का, बंदा नरकि न जाइ॥11॥
कबीर तूँ काहे डरै, सिर परि हरि का हाथ।
हस्ती चढ़ि नहीं डोलिये, कूकर भूसैं जु लाष॥12॥
मीठा खाँण मधूकरी, भाँति भाँति कौ नाज।
दावा किसही का नहीं, बित बिलाइति बड़ राज॥13॥
हस्ती चढ़ि क्या डोलिए। भुसैं हजार।
ख प्रति में इसके आगे यह दोहा है-
हसती चढ़िया ज्ञान कै, सहज दुलीचा डारि।
स्वान रूप संसार है, पड़ा भुसौ झषि माँरि॥15॥)
मोनि महातम प्रेम रस, गरवा तण गुण नेह।
ए सबहीं अह लागया, जबहीं कह्या कुछ देह॥14॥
माँगण मरण समान है, बिरला वंचै कोइ।
कहै कबीर रघुनाथ सूँ, मतिर मँगावै माहि॥15॥
पांडल पंजर मन भवर, अरथ अनूपम बास।
राँम नाँम सींच्या अँमी, फल लागा वेसास॥16॥
कबीर मरौं पै मांगौं नहीं, अपणै तन कै काज।
परमारथ कै कारणै, मोहिं माँगत न आवै लाज॥20॥
भगत भरोसै एक कै, निधरक नीची दीठि।
तिनकू करम न लागसी, राम ठकोरी पीठि॥21॥)
मेर मिटी मुकता भया, पाया ब्रह्म बिसास।
अब मेरे दूजा को नहीं, एक तुम्हारी आस॥17॥
जाकी दिल में हरि बसै, सो नर कलपै काँइ।
एक लहरि समंद की, दुख दलिद्र सब जाँइ॥18॥
पद गाये लैलीन ह्नै, कटी न संसै पास।
सबै पिछीड़ै, थोथरे, एक बिनाँ बेसास॥19॥
गावण हीं मैं रोज है, रोवण हीं में राग।
इक वैरागी ग्रिह मैं, इक गृही मैं वैराग॥20॥
गाया तिनि पाया नहीं, अणगाँयाँ थैं दूरि।
जिनि गाया बिसवास सूँ, तिन राम रह्या भरिपूरि॥21॥
साखी – बिर्कताई कौ अंग
मेरे मन मैं पड़ि गई, ऐसी एक दरार।
फटा फटक पषाँण ज्यूँ, मिल्या न दूजी बार॥1॥
मन फाटा बाइक बुरै, मिटी सगाई साक।
जौ परि दूध तिवास का, ऊकटि हूवा आक॥2॥
चंदन माफों गुण करै, जैसे चोली पंन।
दोइ जनाँ भागां न मिलै, मुकताहल अरु मंन॥3॥
मोती भागाँ बीधताँ, मन मैं बस्या कबोल।
बहुत सयानाँ पचि गया, पड़ि गई गाठि गढ़ोल॥4॥
मोती पीवत बीगस्या, सानौं पाथर आइ राइ।
साजन मेरी निकल्या, जाँमि बटाऊँ जाइ॥5॥)
पासि बिनंठा कपड़ा, कदे सुरांग न होइ।
कबीर त्याग्या ग्यान करि, कनक कामनी दोइ॥4॥
चित चेतनि मैं गरक ह्नै, चेत्य न देखैं मंत।
कत कत की सालि पाड़िये, गल बल सहर अनंत॥5॥
जाता है सो जाँण दे, तेरी दसा न जाइ।
खेवटिया की नाव ज्यूँ, धणों मिलैंगे आइ॥6॥
नीर पिलावत क्या फिरै, सायर घर घर बारि।
जो त्रिषावंत होइगा, तो पीवेगा झष मारि॥7॥
सत गंठी कोपीन है, साध न मानै संक।
राँम अमलि माता रहै, गिणैं इंद्र कौ रंक॥8॥
दावै दाझण होत है, निरदावै निरसंक।
जे नर निरदावै रहैं, ते गणै इंद्र कौ रंक॥9॥
कबीर सब जग हंडिया, मंदिल कंधि चढ़ाइ।
हरि बिन अपनाँ को नहीं, देखे ठोकि बजाइ॥10॥
साखी – सम्रथाई कौ अंग
नाँ कुछ किया न करि सक्या, नाँ करणे जोग सरीर।
जे कुछ किया सु हरि किया, ताथै भया कबीर कबीर॥1॥
कबीर किया कछू न होत है, अनकीया सब होइ।
जे किया कछु होत है, तो करता औरे कोइ॥2॥
जिसहि न कोई तिसहि तूँ, जिस तूँ तिस सब कोइ।
दरिगह तेरी साँईंयाँ, नाँव हरू मन होइ॥3॥
एक खड़े ही लहैं, और खड़ा बिललाइ।
साईं मेरा सुलषना, सूता देइ जगाइ॥4॥
सात समंद की मसि करौं, लेखनि सब बनराइ।
धरती सब कागद करौं, तऊ हरि गुण लिख्या न जाइ॥5॥
बाजण देह बजंतणी, कुल जंतड़ी न बेड़ि।
तुझै पराई क्या पड़ी, तूँ आपनी निबेड़ि॥8॥)
अबरन कौं का बरनिये, मोपै लख्या न जाइ।
अपना बाना बाहिया, कहि कहि थाके माइ॥6॥
झल बाँवे झल दाँहिनैं, झलहिं माँहि ब्यौहार।
आगैं पीछै झलमई, राखै सिरजनहार॥7॥
साईं मेरा बाँणियाँ, सहजि करै ब्यौपार।
बिन डाँडी बिन पालड़ै, तोलै सब संसार॥8॥
कबीर वार्या नाँव परि, कीया राई लूँण।
जिसहिं चलावै पंथ तूँ, तिसहिं भुलावै कौंण॥9॥
कबीर करणी क्या करै, जे राँम न कर सहाइ।
जिहिं जिहिं डाली पग धरै, सोई नवि नवि जाइ॥10॥
जदि का माइ जनमियाँ, कहूँ न पाया सुख।
डाली डाली मैं फिरौं, पाती पाती दुख॥11॥
साईं सूँ सब होत है, बंदे थै कछु नाहिं।
राई थैं परबत करै, परबत राई माहिं॥12॥
रैणाँ दूरां बिछोड़ियां, रहु रे संषम झूरि।
देवल देवलि धाहिणी, देसी अंगे सूर॥13॥
साखी – जीवन मृतक कौ अंग
जीवन मृतक ह्नै रहै, तजै जगत की आस।
तब हरि सेवा आपण करै, मति दुख पावै दास॥1॥
जिन पांऊँ सै कतरी हांठत देत बदेस।
तिन पांऊँ तिथि पाकड़ौ, आगण गया बदेस॥1॥)
कबीर मन मृतक भया, दुरबल भया सरीर।
तब पैडे लागा हरि फिरै, कहत कबीर कबीर॥2॥
कबीर मरि मड़हट रह्या, तब कोइ न बूझै सार।
हरि आदर आगै लिया, ज्यूँ गउ बछ की लार॥3॥
घर जालौं घर उबरे, घर राखौं घर जाइ।
एक अचंभा देखिया, मड़ा काल कौं खाइ॥4॥
मरताँ मरताँ जग मुवा, औसर मुवा न कोइ।
कबीर ऐसैं मरि मुवा, ज्यूँ बहूरि न मरना होइ॥5॥
बैद मुवा रोगी मुवा, मुवा सकल संसार।
एक कबीरा ना मुवा, जिनि के राम अधार॥6॥
मन मार्या ममता मुई, अहं गई सब छूटि।
जोगी था सो रमि गया, आसणि रही विभूति॥7॥
जीवन थै मरिबो भलौ, जौ मरि जानै कोइ।
मरनै पहली जे मरे, तौ कलि अजरावर होइ॥8॥
खरी कसौटी राम की, खोटा टिकैं न कोइ।
राम कसौटी सो टिकै, जो जीवन मृतक होइ॥9॥
आपा मेट्या हरि मिलै, हरि मेट्या सब जाइ।
अकथ कहाणी प्रेम की, कह्या न को पत्याइ॥10॥
निगु साँवाँ वहि जायगा, जाकै थाघी नहीं कोइ।
दीन गरीबी बंदिगी, करता होइ सु होइ॥11॥
दीन गरीबी दीन कौ, दुँदर को अभिमान।
दुँदर दिल विष सूँ भरी, दीन गरीबी राम॥12॥
कबीर नवे स आपको, पर कौं नवे न कोइ।
घालि तराजू तौलिये, नवे स भारी होइ॥14॥
बुरा बुरा सब को कहै, बुरा न दीसे कोइ।
जे दिल खोजौ आपणो, बुरा न दीसे कोइ॥15॥)
कबीर चेरा संत का, दासिन का परदास।
कबीर ऐसे ह्नै रह्या, ज्यूँ पांऊँ तलि घास॥13॥
रोड़ा ह्नै रही बाट का, तजि पादंड अभिमान।
ऐसा जे जन ह्नै रहे, ताहि मिले भगवान॥14॥632॥
रोड़ा भया तो क्या भया, पंथी को दुख देइ।
हरिजन ऐसा चाहिए, जिसी जिमीं की खेह॥18॥
खेह भई तो क्या भया, उड़ि उड़ि लागे अंग।
हरिजन ऐसा चाहिए, पाँणीं जैसा रंग॥19॥
पाणीं भया तो क्या भया, ताता सीता होइ।
हरिजन ऐसा चाहिए, जैसा हरि ही होइ॥20॥
हरि भया तो क्या भया, जैसों सब कुछ होइ।
हरिजन ऐसा चाहिए, हरि भजि निरमल होइ॥21॥
कबीर के दोहे सम्पूर्ण 54000 शब्दों में Part-7
कबीर के दोहे सम्पूर्ण 54000 शब्दों में Part-6
कबीर के दोहे सम्पूर्ण 54000 शब्दों में Part-5
कबीर के दोहे सम्पूर्ण 54000 शब्दों में Part-4
कबीर के दोहे सम्पूर्ण 54000 शब्दों में Part-3
कबीर के दोहे सम्पूर्ण 54000 शब्दों में Part-2
कबीर के दोहे सम्पूर्ण 54000 शब्दों में Part-1
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.
Obrigado, muito legal, seu artigo abriu uma porta para mim. Foi uma grande ajuda para me ajudar a escrever minha tese sobre criptomoedas. Obrigado.